


ShareThis for Joomla!
मौतों की जिम्मेदारी से भागना संभव नहीं होगा
- Details
- Created on Monday, 17 January 2022 08:13
- Written by Shail Samachar
 प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक नीयतन थी या संयोगवश इसकी कोई भी जांच रिपोर्ट आने से पहले ही जिस तरह की राजनीतिक इस पर शुरू हो गयी है उससे कई ऐसे सवाल उठ खड़े हुये हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करना देश हित में नहीं होगा। क्योंकि यदि यह चूक नीयतम है तो उसके प्रायोजकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि संयोगवश हुई इस चूक को अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह और भी निंदनीय है। लोकतंत्र के लिये इससे बड़ा और कोई संकट नहीं हो सकता। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की ही पूर्व जज जस्टिस इन्दु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इसलिए इस जांच की रिपोर्ट आने तक इस पर बहस को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। लेकिन मीडिया के कुछ हिस्सो में इस प्रकरण के बाद राजनीतिक आकलनों का दौर भी शुरू हो गया। पंजाब में इस प्रकरण के बाद भाजपा अमरेंद्र गठबंधन को लाभ और कांग्रेस को नुकसान होने की बात की गयी है वास्तव में क्या होगा यह परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक नीयतन थी या संयोगवश इसकी कोई भी जांच रिपोर्ट आने से पहले ही जिस तरह की राजनीतिक इस पर शुरू हो गयी है उससे कई ऐसे सवाल उठ खड़े हुये हैं जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज करना देश हित में नहीं होगा। क्योंकि यदि यह चूक नीयतम है तो उसके प्रायोजकों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यदि संयोगवश हुई इस चूक को अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यह और भी निंदनीय है। लोकतंत्र के लिये इससे बड़ा और कोई संकट नहीं हो सकता। इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की ही पूर्व जज जस्टिस इन्दु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इसलिए इस जांच की रिपोर्ट आने तक इस पर बहस को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। लेकिन मीडिया के कुछ हिस्सो में इस प्रकरण के बाद राजनीतिक आकलनों का दौर भी शुरू हो गया। पंजाब में इस प्रकरण के बाद भाजपा अमरेंद्र गठबंधन को लाभ और कांग्रेस को नुकसान होने की बात की गयी है वास्तव में क्या होगा यह परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन इस प्रकरण के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मन्त्रीयों और विधायकों ने भाजपा छोड़ना शुरू कर दी है उससे पूरा राजनीतिक परिदृश ही बदलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से पहले उत्तराखंड में भी यही सब कुछ घटना शुरू हुआ था। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भाजपा के प्रभुत्व वाले यही दो राज्य हैं। ऐसी संभावनाएं उभरनी शुरू हो गई हैं कि 2014 में जिस तरह लोग कांग्रेस छोड़कर जाने लगे थे इस बार वैसा ही कुछ भाजपा के साथ घट सकता है। 2014 में जो राजनीतिक परिदृश्य अन्ना आंदोलन से निर्मित हुआ था आज वैसा ही कुछ किसान आंदोलन ने खड़ा कर दिया है। बल्कि इस आंदोलन में हुई सैकड़ों किसानों की मौत ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। फिर इस मुद्दे पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद जब सामने आया कि किसान मोदी के कारण नहीं मरे हैं। प्रधानमंत्री के इस संवाद का किसानों पर क्या असर पड़ा होगा यह अंदाजा लगाना किसी के लिये भी कठिन नहीं है। किसानों की मौत की जिम्मेदारी से सरकार भाग नहीं सकती है।
कुछ लोग किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित मानते हैं इसलिए वह किसानों की मौत के लिए मोदी और उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। इसलिए कृषि कानूनों से जुड़े कुछ बिंदुओं पर बात करना जरूरी हो जाता है। कृषि संविधान के मुताबिक राज्यों का विषय है। एन्ट्री 33 के तहत उत्पादन के भंडारण और वितरण पर केंद्र का भी अधिकार है। लेकिन अन्य मुद्दों पर नहीं। वैसे तो एन्ट्री 33 पर भी विवाद है। इस नाते केंद्र को इस में कानून बनाने का काम अपने हाथ में लेना ही गलत था। फिर यह कानून अध्यादेश के माध्यम से लाये गये। संसद में बाद में रखे गये और वहां बिना बहस के पारित किये गये। यदि इन्हें सामान्य स्थापित प्रक्रिया के तहत लाया जाता तो जैसे ही यह संसद की कार्यसूची में आते तो एकदम सार्वजनिक संज्ञान में आ जाते और इन पर बहस चल पड़ती। जैसा कि इस बार हुआ। कि जैसे ही बैंकिंग अधिनियम में संशोधन की चर्चा सामने आयी तभी बैंक कर्मचारी सड़कों पर आ गये और यह प्रस्तावित संशोधन वहीं पर रुक गया। इसलिए जिस तरीके से यह कृषि कानून लाये गये थे उससे सरकार की नीयत पर शक करने का पर्याप्त आधार बन जाता है।
फिर सरकार ने जमाखोरी और मूल्य बढ़ोतरी पर 1955 से चले आ रहे हैं अपने नियंत्रण के अधिकार को समाप्त करके किसको लाभ पहुंचाया। क्या यह कानून किसी भी आदमी के लिए लाभदायक कहा जा सकता है शायद नहीं। ऐसे में किसानों के पास आंदोलन के अतिरिक्त और क्या विकल्प था। यह कानून कोरोना काल में ही लाने की क्या मजबूरी थी। यह कानून लाने से पहले क्या हरियाणा सरकार द्वारा अदानी समूह को लॉकडाउन के दौरान स्टोरों के लिए भूमि नहीं दी गई थी । अब जब कानून वापिस लिये गये तो उसके बाद अदानी कैपिटल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कृषि ऋणों के लिए पार्टनर क्यों बनाया गया। अब एसबीआई के साथ मिलकर अदानी किसानों को कृषि उपकरणों और बीजों के लिए ऋण देगा। साठ ब्रांचों वाले अदानी से तेईस सौ ब्रांचों वाले एसबीआई को व्यापार में कैसे सहायता मिलेगी। क्या यह सब सरकार की नीयत पर शक करने के लिए काफी नहीं है। क्या इस परिदृश्य में किसान आंदोलन और किसानों की मौतों की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं आ जाती है। यह चुनाव इन्हीं सवालों के गिर्द घूमेगा यह तय है।
क्या सच सिर्फ प्रधानमंत्री ही बोलते हैं
- Details
- Created on Monday, 10 January 2022 15:48
- Written by Shail Samachar
 प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ने मान भी लिया है। दोनों ने ही इस पर अपनी-अपनी जांच भी बिठा दी है। इसी बीच यह मामला सर्वोच्च यायालय में भी पहुंच गया है। केंद और राज्य दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर एतराज उठाये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की ही जांच पर सोमवार तक रोक लगाकर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्टार को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़े सारे दस्तावेजी साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखें। सर्वोच्च न्यायालय के इस दखल के बाद इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विराम लग जाना चाहिये था। लेकिन ऐसा हुआ नही है। यह विवाद जिस तर्ज पर बढ़ाया जा रहा है उससे बड़ा सवाल यह बन गया है इसमें सच कौन बोल रहा है। केंद्र या राज्य सरकार। जनता किस पर विश्वास करे। प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री चन्नी पर। राजनीति भाजपा कर रही है या कांग्रेस। इन सवालों की पड़ताल करने के लिये सबसे पहले यह जानना और समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्या है। जब देश ने एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधनमंत्री को सुरक्षा चुक के कारण खो दिया था तब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये एक अधिनियम लाकर एसपीजी का गठन किया था। इस अधिनियम के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये एसपीजी ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी कदम कोई भी फैसला लेने का अंतिम अधिकार एसपीजी का ही रहता है। अन्य सारी एजेंसियां इस संबंध में उसी के निर्देशों की अनुपालना करती है। इस व्यवस्था के परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारे पक्ष आ जायेंगे यह तय है और सारी असलियत सामने आ जायेगी।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ने मान भी लिया है। दोनों ने ही इस पर अपनी-अपनी जांच भी बिठा दी है। इसी बीच यह मामला सर्वोच्च यायालय में भी पहुंच गया है। केंद और राज्य दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर एतराज उठाये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की ही जांच पर सोमवार तक रोक लगाकर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्टार को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़े सारे दस्तावेजी साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखें। सर्वोच्च न्यायालय के इस दखल के बाद इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विराम लग जाना चाहिये था। लेकिन ऐसा हुआ नही है। यह विवाद जिस तर्ज पर बढ़ाया जा रहा है उससे बड़ा सवाल यह बन गया है इसमें सच कौन बोल रहा है। केंद्र या राज्य सरकार। जनता किस पर विश्वास करे। प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री चन्नी पर। राजनीति भाजपा कर रही है या कांग्रेस। इन सवालों की पड़ताल करने के लिये सबसे पहले यह जानना और समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्या है। जब देश ने एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधनमंत्री को सुरक्षा चुक के कारण खो दिया था तब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये एक अधिनियम लाकर एसपीजी का गठन किया था। इस अधिनियम के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये एसपीजी ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी कदम कोई भी फैसला लेने का अंतिम अधिकार एसपीजी का ही रहता है। अन्य सारी एजेंसियां इस संबंध में उसी के निर्देशों की अनुपालना करती है। इस व्यवस्था के परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारे पक्ष आ जायेंगे यह तय है और सारी असलियत सामने आ जायेगी।
यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक दूसरी बार हुई है। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री को एक आयोजन में शामिल होने के लिए अमेठी विश्वविद्यालय के परिसर में जाना था यहां पर जाने के लिये प्रधानमंत्री का काफिला रास्ता भूल गया। यह रास्ता भूलना भटकना सुरक्षा के लिये गंभीर चूक थी। लेकिन तब इस चूक के लिये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। संबंधित एसपी ने इस चूक के लिये दो पुलिसकर्मियों को निलंबित करके मामले की जांच पूरी कर दी थी। उस समय यह सुरक्षा चूक अखबारों की खबर तक नहीं बनी। आज यदि पंजाब के प्रसंग को यह कहकर चर्चा का विषय न बनाया होता ‘‘ कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं सुरक्षित वापस आ गया हूं ’’ तो शायद यह पुराने प्रसंग सामने न आते। आज इस प्रकरण के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक के सबके आचरण के वह प्रसंग सामने आ गये हैं कि अपने विरोधियों की बात को किस धैर्य के साथ वह सुनते थे और उनके विरोध के अधिकार की कितनी रक्षा करते थे। पंडित नेहरू का बिहार का सैयद शहाबुद्दीन प्रकरण आज अचानक चर्चा में आ गया है। बिहार में पंडित नेहरू को काले झंडे दिखाने वाले शहाबुद्दीन कैसे लोक सेवा आयोग के सेकंड टापर बने थे। डॉ. मनमोहन सिंह ने जेएनयू के छात्रों के विरोध का कैसे जवाब दिया और उन्हें दिये गये नोटिस कैसे वापस करवाये गये। किस तरह राजीव गोस्वामी के आत्मदाह प्रकरण में अस्पताल जाकर उनका हाल पूछा और विदेश तक उसका इलाज करवाने के निर्देश दिये। यह सब आज याद किया जाने लगा है। क्योंकि इन्होंने इस विरोध के लिये इनके खिलाफ देशद्रोह के मामले नहीं बनवाये।
आज मतभिन्नता के लिये भाजपा शासन में केंद्र से लेकर राज्यों तक कहीं कोई स्थान नहीं बचा है। भिन्न मत रखने वाले को व्यक्तिगत दुश्मन मानकर उसे हर तरह से कुचलने का प्रयास किया जाता है। अभी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री का किसानों की मौतों को लेकर जो संवाद सामने आया है उसमें 500 किसानों की मौत पर यह कहना कि यह लोग मेरे लिये या मेरे कारण नहीं मरे हैं। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का इससे बड़ा नकारात्मक पक्ष और कुछ नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही जिस तरह से पंजाब सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है उससे पुराने सारे प्रकरण अनचाहे की तुलना में आ गये हैं। आज जनता को किसी भी ऐसे प्रयास से गुमराह नहीं किया जा सकता। क्योंकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने हर आदमी को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि यह सरकार केवल कुछ बड़े पूंजीपतियों के हित की ही रक्षा कर रही है। आम आदमी को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही उलझाये रखना चाहती है।
क्या कोरोना का राजनीतिक उपयोग हो रहा है?
- Details
- Created on Monday, 03 January 2022 17:32
- Written by Shail Samachar




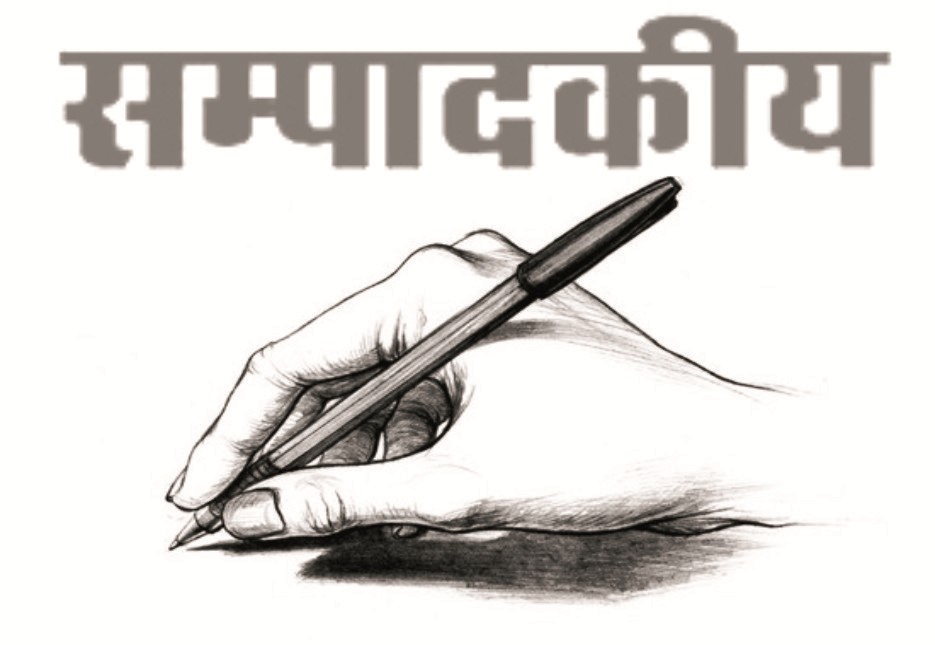
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाकर इस महामारी से निपटने का पहला कदम उठाया था। लॉकडाउन की घोषणा अचानक हुई थी। लोगों की लॉकडाउन झलेने की कोई तैयारी नहीं थी। जबकि महामारी अधिनियम 1897 में यह प्रावधान है कि जब कोई बीमारी सरकार के आकलन में महामारी लगे और उससे निपटने के लिये अलग से कुछ कदम उठाने पड़े तो उसके लिए जनता को सार्वजनिक रूप से अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। लेकिन लॉकडाउन लगाते समय कुछ नहीं किया गया। लॉकडाउन में किस तरह का नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ा है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नवम्बर 2016 में की गयी नोटबंदी से जो नुकसान आर्थिकी को पहुंचा था लॉकडाउन ने उसे कई गुना बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त बाकी सारी आर्थिक गतिविधियां शुन्य हो गयी। 2020 में कोरोना के लिये कोई वैक्सीन या अन्य कोई दवाई बाजार में नहीं आयी। आज भी इसकी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष जनवरी से जो वैक्सीन लगाई जा रही है वह केवल एक प्रतिरोधक उपाय है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी केवल छः माह तक कारगर है। इसके बाद पुनः इसकी डोज लेनी पड़ेगी। ऐसा कब तक करते रहना पड़ेगा इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वैक्सीन की इस व्यवहारिक स्थिति के कारण ही सर्वाच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र देकर यह कहा है की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं किया गया है। इसे एैच्छिक ही रखा गया है। 2020 में आरोग्य सेतु ऐप आया था। इसको लेकर कितने दावे किये गये थे और उन्हीं दावों के आधार पर इसे अनिवार्य बना दिया गया था। लेकिन जब एक आर.टी.आई. में इससे जुड़ी जानकारियां मांगी गयी तब ऐप को लेकर ही अनभिज्ञता जता दी गयी। इससे आम आदमी के विश्वास को कितना आघात पहुंचा है इसका अंदाजा लगाना कठिन है।
1897 में महामारी अधिनियम आने के बाद से लेकर आज तक का रिकार्ड यह बताया है कि हर दस-बारह वर्ष के अंतराल पर कोई न कोई महामारी आती रही है लेकिन इससे निपटने के इस तरह के उपाय पहली बार किये गये हैं जिनमें शुरुआत में ही यह कहा गया कि अस्पताल भी ना जायें। इस निर्देश में यह ध्यान नहीं रखा गया कि जो लोग आ.ेपी.डी. में आ रहे हैं या अस्पताल में दाखिल होकर इलाज करवा रहे हैं और अब उनका इलाज बंद हो गया है उनमें से यदि कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका बचाव कैसे होगा। आज तक इस पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि जब 24 मार्च को लॉकडाउन के कारण अस्पताल भी बंद हो गये थे तब अस्पताल आने वाले कितने लोग संक्रमित हुए और उनकी स्थिति क्या रही। जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद एक याचिका सर्वाच्च न्यायालय में डॉ कुनाल साहा की आई थी उसमें संभावित प्रस्तावित दवाइयों और वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कुछ चिन्ताएं व्यक्त की गयी थी। जिनका आज तक जवाब नहीं आया है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों और फिर कुछ पूर्व वरिष्ठ नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कुछ जानकारीयां इस महामारी को लेकर मांगी थी जिनका जवाब नहीं आया है। अब डॉक्टर जैकब पुलियेल की याचिका पर यह शपथ पत्र आ गया कि वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं की गयी है यह एैच्छिक है। लेकिन व्यवहार में जिस तरह की बंदिशों के आदेश/निर्देश सामने आ रहे हैं वह रिकॉर्ड पर आ चुकी स्थिति से एकदम भिन्न है। इस भिन्नता के कारण ही यह आशंकाएं उभर रही हैं कि कहीं इस महामारी का कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं उठाया जा रहा है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के आंकड़े संसद में गृह विभाग की ओर से हर वर्ष रखे जाते हैं। क्योंकि हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है। मृत्यु के इन आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से इसमें प्रतिवर्ष दस बारह लाख की बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में यह आंकड़ा 69 लाख था और आज भी यह 7.27 प्रति हजार है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्यवहार और प्रचार में कितना अंतर है।
क्या चुनाव टालने की भूमिका बनाई जा रही है
- Details
- Created on Monday, 27 December 2021 04:00
- Written by Shail Samachar




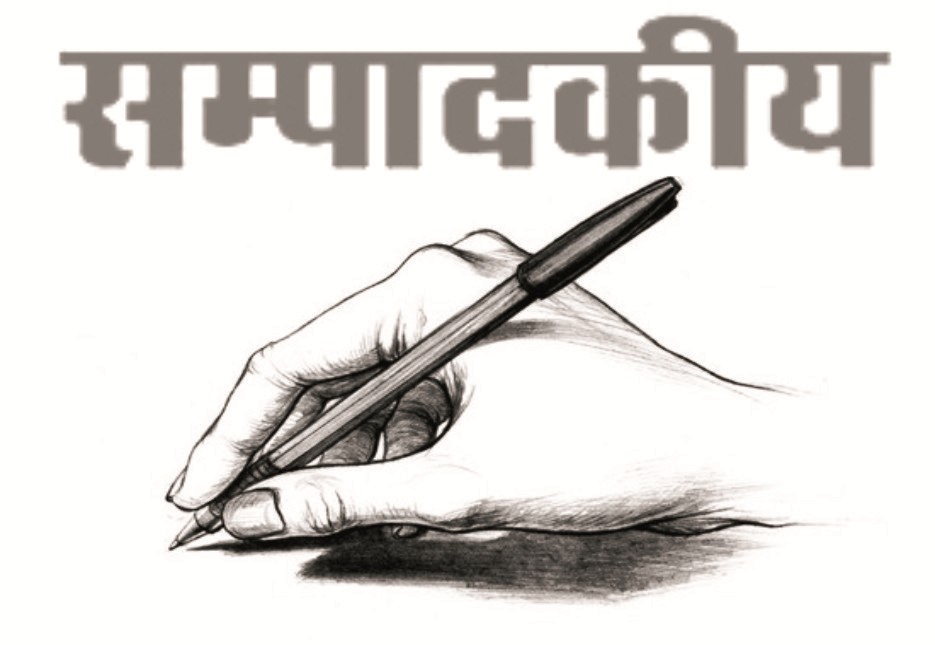
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या सरकार पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को टालने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश की चुनावी अहमियत इसी धारणा से पता चल जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 और 2019 के चुनावों के बाद यह कहा जाने लगा था कि उसे वहां पर कोई चुनौती ही नहीं बनी है वहां पर आज जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जनसभाओं में उमड रही है उससे भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ उभरना शुरू हो गयी हैं। क्योंकि इसी अनुपात में अब प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नड्डा की सभाओं में खाली कुर्सियां दिखनी शुरू हो गयी है। प्रियंका और राहुल के प्रयासों से कांग्रेस ने मुकाबले को तिकोना बना दिया है। फिर अयोध्या, काशी और मथुरा के प्रयोगों से भी धार्मिक और जातीय धुव्रीकरण नहीं बन पाया है। लखीमपुर खीरी काण्ड के बाद भी किसान आंदोलन में हिंसा न हो पाना इसी कड़ी में देखा जा रहा है। बल्कि इस काण्ड पर आई एस.आई.टी. की रिपोर्ट के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भाजपा का नैगेटिव बनता जा रहा है। राम मंदिर के लिये की गई जमीन में लगे घोटाले के आरोपों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। महंगाई और बेरोजगारी से जिस कदर आम आदमी पीड़ित हो उठा है उससे किसी भी तरह के धुव्रीकरण के प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। ऊपर से अब कृषि मंत्री तोमर का यह ब्यान कि सरकार कृषि कानूनों को लेकर फिर से एक प्रयास करेगी से स्थिति और उलझ गयी है। बल्कि इस ब्यान के बाद ममता बनर्जी के लिये भी अदानी के साथ बन रहे रिश्तों पर जवाब देना कठिन हो जायेगा। इस सब को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि यू.पी. में भाजपा की राह लगातार कठिन होती जा रही है और इससे एकदम बाहर निकलने के लिए ओमीक्राम के खतरे के नाम पर चुनाव टालने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह जाता है।
पांच राज्यों के लिये हो रहे चुनावों को लेकर सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक कहीं भी भाजपा सुखद स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा के कई मंत्री और विधायक कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। पंजाब में भाजपा को उस अमरिंदर सिंह का दामन थामना पड़ रहा है जो कांग्रेस छोड़ने के बाद पटियाला में ही अपने आदमी को मेयर का चुनाव नहीं जीतवा पाये। बंगाल की हार से प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत साख को जो धक्का पहुंचा है उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाये हैं। इस लिए अभी ओमीक्राम के नाम पर छः माह के लिए चुनाव टालने की भूमिका बनाई जा रही है। कुछ राज्यों द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया जाना इसी दिशा का प्रयास है। यदि एक बार चुनाव टाल दिये जाते हैं तो इन राज्यों में अपने आप ही राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति आ जायेगी। जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में महामारी अधिनियम और महामारी की व्यवहारिकता को लेकर एक चर्चा की आवश्यकता हो जाती है और इसे अगले अंक में उठाया जायेगा।
घातक होगा सार्वजनिक सवालों पर बहस से भागना
- Details
- Created on Wednesday, 22 December 2021 03:55
- Written by Shail Samachar




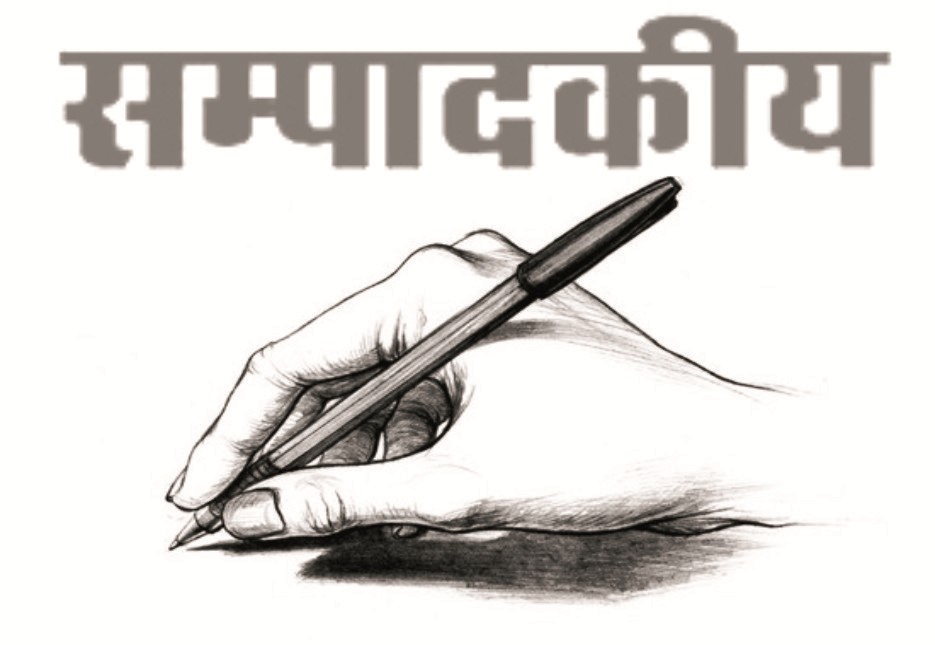
बैंकिंग देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में 2014 -15 से 2020-2021 तक कमर्शियल बैंकों का एनपीए दो लाख करोड़ से बढ़कर 25.24 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इनमें रिकवरी केवल 593956 करोड़ ही हो पायी है जबकि 10,72116 करोड़ की कर्ज माफ कर दिया गया। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए इसी अवधि में 1904350 करोड़ को पहुंच गया जिसमें रिकवरी सिर्फ 448784 करोड़ और इसमें 807488 करोड़ का कर्ज इसमें माफ किया गया है। यह सारे आंकड़े आरबीआई से 13.8.21 की एक आरटीआई के माध्यम से सामने आये हैं। इन आंकड़ों से यह सामने आया है कि इस सरकार के कार्यकाल में करीब बीस लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। इसी कर्ज माफी का परिणाम है कि बैंकों में जमा पूंजी पर लगातार ब्याज कम होता जा रहा है और बैंकों की सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी भी इसी सबका परिणाम है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दिन यह चिन्हित अदारे पूरी तरह से प्राइवेट सैक्टर के हवाले हो जायेंगे उस दिन महंगाई और बेरोजगारी का आलम क्या होगा।
इस सारे खुलासे के बाद यह सवाल जवाब मांगते हैं कि क्या इस सब पर देश के अंदर एक सार्वजनिक बहस नहीं हो जानी चाहिये थी? सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करके कितनी देर देश को चलाया जा सकेगा? जिस देश के बैंकों की हालत यहां तक पहुंच गयी है कि 22219 ब्रांचों वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 60 ब्रांचों वाले अदानी कैपिटल को अपना लोन पार्टनर बनाना पड़ा है यदि वहां के बैंक प्राइवेट हाथों में चले जायें तो आम आदमी का पैसा कितनी देर सुरक्षित रह पायेगा? प्राइवेट बैंक गरीब आदमी को क्यों और किन शर्तों पर कर्ज उपलब्ध करावायेगा? क्या इस वस्तुस्थिति का देर-सवेर हर आदमी पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इन सवालों को हिन्दू-मुस्लिम करके नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरीडोर और मथुरा में कृष्ण मूर्ति रखने से महंगाई और बेरोजगारी के प्रश्न हल हो जायेंगे? आज जो नेता और राजनीतिक दल इन सवालों पर मौन धारण करके बैठ गये हैं क्या उनके हाथों में देश सुरक्षित रह पायेगा? क्या ऐसे परिदृश्य में आज संसद से लेकर हर गली चौराहे तक इन सवालों पर बहस नहीं होनी चाहिये?
घातक होगा सार्वजनिक सवालों पर बहस से भागनावोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का विधेयक लोकसभा में बिना बहस के पारित हो गया है। इसे चुनाव सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। इस विधेयक को लोकसभा में लाये जाने से पहले चुनाव आयोग और पीएमओ के बीच एक बैठक होने का विवाद भी उभरा था। इस विवाद के परिदृश्य में यदि इस चुनाव सुधार पर संसद में बहस हो जाती तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा हो नही पाया। शायद इस सरकार की यह संस्कृति ही बन गयी है कि विपक्ष की कोई भी बात सुननी ही नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री भी केवल अपने मन की ही बात जनता को सुनाने के सिद्धांत पर चलते आ रहे हैं उनकी सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। दर्जनों उदाहरण इस चलन के नोटबंदी से लेकर कृषि कानूनों के पास होने से लेकर उनके वापिस होने तक के मौजूद हैं। इस चलन में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप हर बार हर समय ठीक नहीं हो सकते। आर्थिक क्षेत्र में जितने भी फैसले लिये गये हैं उनका ठोस लाभ केवल 10ः समृद्ध लोगों को ही मिला है और बाकी के नब्बे प्रतिश्त के तो साधन ही कितने चले गये हैं। सरकार जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों की पक्षधर होकर रह गयी है उसका सबसे बड़ा प्रमाण सरकार की विनिवेश योजना है। जिसके तहत अच्छी आय देने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा उत्पादन और ट्रांसमिशन, तेल और गैस पाइपलाइनज, टेलीकॉम इंफ्र्रास्ट्रक्चर तथा खनिज और खानों को निजी क्षेत्र में सौंपकर इससे छःलाख करोड़ जुटाने की योजना है। इसी विनिवेश के तहत सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट सैक्टर को देने का विधेयक लाया जा रहा था जिसे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका से टाल दिया गया। लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अदानी कैपिटल की हुई हिस्सेदारी से इसका श्रीगणेश कर दिया गया है। बैंकिंग देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में 2014 -15 से 2020-2021 तक कमर्शियल बैंकों का एनपीए दो लाख करोड़ से बढ़कर 25.24 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इनमें रिकवरी केवल 593956 करोड़ ही हो पायी है जबकि 10,72116 करोड़ की कर्ज माफ कर दिया गया। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए इसी अवधि में 1904350 करोड़ को पहुंच गया जिसमें रिकवरी सिर्फ 448784 करोड़ और इसमें 807488 करोड़ का कर्ज इसमें माफ किया गया है। यह सारे आंकड़े आरबीआई से 13.8.21 की एक आरटीआई के माध्यम से सामने आये हैं। इन आंकड़ों से यह सामने आया है कि इस सरकार के कार्यकाल में करीब बीस लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया। इसी कर्ज माफी का परिणाम है कि बैंकों में जमा पूंजी पर लगातार ब्याज कम होता जा रहा है और बैंकों की सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। महंगाई और बेरोजगारी भी इसी सबका परिणाम है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दिन यह चिन्हित अदारे पूरी तरह से प्राइवेट सैक्टर के हवाले हो जायेंगे उस दिन महंगाई और बेरोजगारी का आलम क्या होगा। इस सारे खुलासे के बाद यह सवाल जवाब मांगते हैं कि क्या इस सब पर देश के अंदर एक सार्वजनिक बहस नहीं हो जानी चाहिये थी? सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट सैक्टर के हवाले करके कितनी देर देश को चलाया जा सकेगा? जिस देश के बैंकों की हालत यहां तक पहुंच गयी है कि 22219 ब्रांचों वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 60 ब्रांचों वाले अदानी कैपिटल को अपना लोन पार्टनर बनाना पड़ा है यदि वहां के बैंक प्राइवेट हाथों में चले जायें तो आम आदमी का पैसा कितनी देर सुरक्षित रह पायेगा? प्राइवेट बैंक गरीब आदमी को क्यों और किन शर्तों पर कर्ज उपलब्ध करावायेगा? क्या इस वस्तुस्थिति का देर-सवेर हर आदमी पर असर नहीं पड़ेगा? क्या इन सवालों को हिन्दू-मुस्लिम करके नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरीडोर और मथुरा में कृष्ण मूर्ति रखने से महंगाई और बेरोजगारी के प्रश्न हल हो जायेंगे? आज जो नेता और राजनीतिक दल इन सवालों पर मौन धारण करके बैठ गये हैं क्या उनके हाथों में देश सुरक्षित रह पायेगा? क्या ऐसे परिदृश्य में आज संसद से लेकर हर गली चौराहे तक इन सवालों पर बहस नहीं होनी चाहिये?



