


ShareThis for Joomla!
केन्द्र की नीतियों पर सीधा प्रश्न चिन्ह है यह चुनाव परिणाम
- Details
- Created on Tuesday, 29 October 2019 08:25
- Written by Shail Samachar
 अभी हुए दो राज्यों के विधान सभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा को जनता ने सरकार बनाने लायक बहुमत नही दिया है। महाराष्ट्र में भी 2014 से कम सीटें मिली हैं। अनय राज्यों में भी जहां जहां उप चुनाव हुए हैं वहां पर अधिकांष में सतारूढ़ सरकारों कें पक्ष में ही लोगों ने मतदान किया हैं । यह चुनाव पांच माह पहले हुये लोकसभा चुनावों के बाद हुए हैं और इनके परिणाम उनसे पूरी तरह उल्ट आये हैं। क्योंकि लोकसभा में हरियाणा की सभी दस सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और इसी जीत के दम पर विधान सभा चुनावों में 90 में से कम से कम 75 सीटे जीतने का लक्ष्य घोषित किया था। अंबानी और अदानी की मलकीयत वाला मीडिया तो हरियाणा में कांग्रेस को चार पांच और महाराष्ट्र में आठ से दस सीटें दे रहा था। इसी मीडिया के प्रभाव में अधिकांश सोशल मीडिया भी इसी तरह के आकलन परोसने लग गया था। ऐसा शायद इसलिये था कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष को ऐसा अप्रत्याशित हार मिली थी जिसका किसी को भी अनुमान नही था। इस हार से विपक्ष एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर ही हताशा में चला गया था। एक बार फिर विपक्षी दलों के लोग पासे बदलने लग गये थे। इसी के साथ ईडी और सीबीआई की सक्रियता भी बढ़ गई कई महत्वपूर्ण नेताओं को जेल के दरवाजे दिखा दिये गये। कुल मिलाकर नयी स्थिति यह उभरती चली गई कि भाजपा अब कांग्रेस मुक्त नही बल्कि विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखने लग गई थी । विपक्ष की एकजुटता की संभावनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। कांग्रेस में राहूल गांधी एक तरह से हार के बाद अकेले पड़ गये थे क्योंकि हार कि जिम्मेदारी लेने के लिये पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़े नही हुआ। राहूल को अकेले ही यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी और त्याग पत्र देना पड़ा। इस त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के ही कई नेता अपरोक्ष में उनके खिलाफ मुखर होने लग गये थे। अन्य विपक्षी दल तो एकदम पूरे सीन से ही गायब हो गये थे। भाजपा संघ को कोई चुनौती देने वाला नजर नही आ रहा था।
अभी हुए दो राज्यों के विधान सभा चुनावों में हरियाणा में भाजपा को जनता ने सरकार बनाने लायक बहुमत नही दिया है। महाराष्ट्र में भी 2014 से कम सीटें मिली हैं। अनय राज्यों में भी जहां जहां उप चुनाव हुए हैं वहां पर अधिकांष में सतारूढ़ सरकारों कें पक्ष में ही लोगों ने मतदान किया हैं । यह चुनाव पांच माह पहले हुये लोकसभा चुनावों के बाद हुए हैं और इनके परिणाम उनसे पूरी तरह उल्ट आये हैं। क्योंकि लोकसभा में हरियाणा की सभी दस सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और इसी जीत के दम पर विधान सभा चुनावों में 90 में से कम से कम 75 सीटे जीतने का लक्ष्य घोषित किया था। अंबानी और अदानी की मलकीयत वाला मीडिया तो हरियाणा में कांग्रेस को चार पांच और महाराष्ट्र में आठ से दस सीटें दे रहा था। इसी मीडिया के प्रभाव में अधिकांश सोशल मीडिया भी इसी तरह के आकलन परोसने लग गया था। ऐसा शायद इसलिये था कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष को ऐसा अप्रत्याशित हार मिली थी जिसका किसी को भी अनुमान नही था। इस हार से विपक्ष एक तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर ही हताशा में चला गया था। एक बार फिर विपक्षी दलों के लोग पासे बदलने लग गये थे। इसी के साथ ईडी और सीबीआई की सक्रियता भी बढ़ गई कई महत्वपूर्ण नेताओं को जेल के दरवाजे दिखा दिये गये। कुल मिलाकर नयी स्थिति यह उभरती चली गई कि भाजपा अब कांग्रेस मुक्त नही बल्कि विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखने लग गई थी । विपक्ष की एकजुटता की संभावनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। कांग्रेस में राहूल गांधी एक तरह से हार के बाद अकेले पड़ गये थे क्योंकि हार कि जिम्मेदारी लेने के लिये पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़े नही हुआ। राहूल को अकेले ही यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी और त्याग पत्र देना पड़ा। इस त्याग पत्र के बाद कांग्रेस के ही कई नेता अपरोक्ष में उनके खिलाफ मुखर होने लग गये थे। अन्य विपक्षी दल तो एकदम पूरे सीन से ही गायब हो गये थे। भाजपा संघ को कोई चुनौती देने वाला नजर नही आ रहा था।
भाजपा ने इसी परिदृश्य का लाभ उठाते हुये तीन तलाक विधेयक को फिर से संसद में लाकर पारित करवा लिया। इसके बाद जम्मू- कश्मीर से धारा 370 और 35 A को हटाकर जम्मू- कश्मीर को दो केन्द्र शासित राज्यों में बांट दिया। पूरी घाटी में हर तरह के नीगरिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। पूरा प्रदेश एक तरह से सैनिक शासन के हवाले कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी नागरिक अधिकारों के हनन को लेकर आयी याचिकाओं पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। जिन बुद्धिजीवियों ने भीड़ हिसां के खिलाफ राष्ट्रपति को सामूहिक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया था उनक खिलाफ पटना में एक अदालत के आदेशों पर एफ आई आर तक दर्ज कर दी गयी। इससे सार्वजनिक भय का वातावरण और बढ़ गया। नवलखा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के करीब आधा दर्जन न्यायाधीशों द्वारा मामले की सुनवाई से अपने को अलग करना न्यायपालिका की भूमिका पर अलग से सवाल खड़े करता है। धारा 370 हटाने पर विश्व समुदाय के अधिकांश देशों द्वारा समर्थन का दावा इसी का परिचायक था कि ‘‘ King does no Wrong ’’ स्वभाविक है कि जब इस तरह के एक पक्षीय राजनीतिक वातावरण में कोई चुनाव आ जाये तो उनके परिणाम भी एकतरफा ही रहने का दावा करना कोई आश्चर्यजनक नही लगेगा।
ऐसे राजनीतिक परिदृश्य क बाद भी यदि जनता हरियाणा जैसे जनादेश दे तो यह अपने में एक महत्वपूर्ण चिन्तन का विषय बन जाता है। जब सब कुछ सता पक्ष क पक्ष में जा रहा था तो ऐसा क्या घट गया कि जनता विपक्ष के अभाव में भी ऐसा जनादेश देने पर आ गई। इसकी अगर तलाश की जाये तो यह सामने आता हैं कि राजनीतिक फैसलों का मुखौटा ओढ़कर जो आर्थिक फैसले लिये वह जनता पर भारी पड़ गये। जो सरकार चुनाव की पूर्व सन्धया पर किसानों को छः छः हजार प्रतिवर्ष देकर लुभा रही थी उसे सरकार बनते ही रिजर्व बैंक से 1.76 लाख करोड़ लेना पडा इसके बाद 1.45 लाख करोड़ का राहत पैकेज कारपोरेट जगत को देना पड़ा और इसक बावजूद भी आर्थिक मन्दी में कोई सुधार नही आ पाया। आटोमोबाईल और टैक्सटाईल क्षेत्रों में कामगारों की छटनी नही रूक पायी उनके उतपादो की बिक्री नही बढ़ पायी। रेलवे बी एस एन एल और एम टी एन एल मे विनिवेश की घोषणाओं से रोजगार के संकट उभरने के संकेतो से एकदम महंगाई का बढ़ना आम आदमी क लिये काफी था। उसे इतनी बात तो समझ आ ही जाती है कि मंहगाई और बेरोजगारी पर नियन्त्रण रखना हमेशा समय का सतारूढ़ सरकार का दायित्व होता है। जिसमें यह सरकार लगातार असफल होती जा रही है। आर्थिक क्षेत्र की असफलताओं का ढकने के लिये जब प्रधानमंत्री ने विधान सभा चुनावों में विपक्ष को यह कह कर चुनौति दी कि यदि उसमें साहस है तो वह 370 का फिर लागू करने का दावा करे। इन विधान समभा चुनावों में धारा 370 विपक्ष का कोई मुद्दा ही नही था क्योंकि इसका चुनावों के साथ कोई सीधा संबंध ही नही था। लेकिन प्रधानमंत्री का विपक्ष को इस मुद्दे पर लाने का प्रयास करना ही यह स्पष्ट करता है कि सता पक्ष के पास अब ऐसा कुछ नही बचा है जो आर्थिक मन्दी पर भारी पड़ जाये । क्योंकि सारे धर्म स्थलों को भी यदि राम मन्दिर बना दिया जाये और सारे गैर हिन्दु भी यदि हिन्दु बन जाये तो भी बेरोजगारी और मंहगाई से जनता को निजात नही मिल पायेगी। क्योंकि 3000 करोड़ खर्च करके पटेल की प्रतिमा स्थापित करने से यह समस्याएं हल नही हो सकती यह तह है।
इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के आर्थिक परिवेश ने हर आदमी को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी जान चुका है कि कल तक स्वदेशी जागरण मंच खडा करके एफ डी आई का विरोध करने वाला सता पक्ष जब रक्षा जैसे क्षेत्र में एफ डी आई को न्योता दे चुका है तो यह प्रमाणित हो जाता है कि यह सब उसकी राजनीतिक चालबाजी से अधिक कुछ नही था। जंहा वैचारिक विरोध को देशद्रोह की संज्ञा दी जायेगी तो ऐसी राजनीतिक मान्यताएं ज्यादा देर तक टिकी नही रह सकती हैं। आज देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी इस तरह के मुद्दों पर मुखर होने लग गये हैं और केन्द्र सरकार से उन अधिकारियों को केंन्द्र से वापिस राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है जो आंख बन्द करके उसकी हां में हां मिलाने को तैयार नही है। आज विपक्ष को इन उभरते संकेतों को समझने और अपनी हताशा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। क्योंकि पांच माह में ही इस तरह का खंडित जनादेश किसी भी गणित में सता के पक्ष में नही जाता है शायद इसीलिये प्रधानमंत्री को हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रीयों के साथ खड़ा होना पड़ा है कि कहीं वह इस जनादेश का ठिकरा केन्द्र के सिर न फोड़ दें।
क्या बैंको में आम आदमी का पैसा सुरक्षित है?
- Details
- Created on Monday, 21 October 2019 13:44
- Written by Shail Samachar
 पिछले कुछ अरसे से देश की आर्थिक स्थिति लगातार चिन्तन और चिन्ता का विषय बनी हुई है। जब से पी एम सी और लक्ष्मी विलास बैंक के कारोबार पर आरबीआई ने रोक लगायी तब से यह चिन्ता और बढ़ गयी है। लोगों में यह भय व्याप्त हो गया है कि बैकों में रखा उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। बैंकों की यह स्थिति लगातार बढ़ते एनपीए और फ्राड की घटनाओं के कारण हो रही है। संसद के मानसून सत्र में यह आंकड़ा सामने आ चुका है कि बैंकों का साढ़े आठ लाख करोड़ का एनपीए राइट आॅफ कर दिया गया है। इसी के साथ यह भी सामने आया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब पौने दो लाख करोड़ के बैंक फ्राड घट गये हैं जबकि डा.मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 से 2014 तक कुल 29000 हजार करोड़ के बैंक फ्राड हुए हैं। लेकिन इसकी तुलना में मोदी सरकार में तो वित्तिय वर्ष 2019 -20 के पहले तीन माह में ही 31000 करोड़ से कुछ अधिक के फ्राड घट गये हैं। लेकिन मोदी सरकार लोगों की इस चिन्ता को लेकर कोई आश्वासन नही दे पा रही है। आरबीआई इस अस्पष्ट स्थिति के कारण आर्थिक विकास दर का कोई एक लक्ष्य तय नही कर पायी है। इसी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ही सरकार को रिर्जव बैंक से सुरक्षित धन लेना पड़ा है और कारपोरेट जगत को 1.45 लाख करोड़ की कर राहत देनी पड़ी है। इसी के परिणामस्वरूप सरकार को अपने उपक्रम निजिक्षेत्र को देने की योजना बनानी पड़ी है। विनिवेश मंत्रालय इस काम पर लगा हुआ है। यह तय है कि जिस दिन बड़े उपक्रम प्राईवेट सैक्टर में चले जायेंगे तभी बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट सामने आयेगा।
पिछले कुछ अरसे से देश की आर्थिक स्थिति लगातार चिन्तन और चिन्ता का विषय बनी हुई है। जब से पी एम सी और लक्ष्मी विलास बैंक के कारोबार पर आरबीआई ने रोक लगायी तब से यह चिन्ता और बढ़ गयी है। लोगों में यह भय व्याप्त हो गया है कि बैकों में रखा उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं। बैंकों की यह स्थिति लगातार बढ़ते एनपीए और फ्राड की घटनाओं के कारण हो रही है। संसद के मानसून सत्र में यह आंकड़ा सामने आ चुका है कि बैंकों का साढ़े आठ लाख करोड़ का एनपीए राइट आॅफ कर दिया गया है। इसी के साथ यह भी सामने आया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक करीब पौने दो लाख करोड़ के बैंक फ्राड घट गये हैं जबकि डा.मनमोहन सिंह की सरकार में 2009 से 2014 तक कुल 29000 हजार करोड़ के बैंक फ्राड हुए हैं। लेकिन इसकी तुलना में मोदी सरकार में तो वित्तिय वर्ष 2019 -20 के पहले तीन माह में ही 31000 करोड़ से कुछ अधिक के फ्राड घट गये हैं। लेकिन मोदी सरकार लोगों की इस चिन्ता को लेकर कोई आश्वासन नही दे पा रही है। आरबीआई इस अस्पष्ट स्थिति के कारण आर्थिक विकास दर का कोई एक लक्ष्य तय नही कर पायी है। इसी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ही सरकार को रिर्जव बैंक से सुरक्षित धन लेना पड़ा है और कारपोरेट जगत को 1.45 लाख करोड़ की कर राहत देनी पड़ी है। इसी के परिणामस्वरूप सरकार को अपने उपक्रम निजिक्षेत्र को देने की योजना बनानी पड़ी है। विनिवेश मंत्रालय इस काम पर लगा हुआ है। यह तय है कि जिस दिन बड़े उपक्रम प्राईवेट सैक्टर में चले जायेंगे तभी बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट सामने आयेगा।
देश व्यवहारिक रूप से इस संकट के दौर से गुज़र रहा है लेकिन अभी तक सरकार इस स्थिति को स्वीकार करने के लिये तैयार नही हो रही है। सरकार अभी भी देश को धारा 370 और 35 ए तथा तीन तलाक जैसे मुद्दों के गिर्द ही घुमाये रखने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री और गृहमन्त्री विधान सभाओं के चुनावों को भी इन्ही मुद्दों के गिर्द केन्द्रित रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बढ़ती बेरोज़गारी और मंहगाई के सामने सरकार के पास और कुछ भी आम आदमी के सामने परोसने के लिये नहीं है। बेरोज़गारी और मंहगाई दो ऐसे मुद्दे हैं जो देश की 90ः आबादी को सीेधे प्रभावित करते हैं। सरकार आर्थिक स्थिति के लिये अभी कांग्रेस को ही दोषी ठहराने का प्रयास कर रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी बहुत कुछ ब्यान कर जाती है कि वहां पर सरकार नही जंगल राज है।
इस परिदृश्य में यह सवाल अब लगातार चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि आखिर इस सबका अन्त होगा क्या। आर्थिक मंदी से निकट भविष्य में बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि सरकार का हर उपाय केवल उद्योगपति को ही लाभ पहुंचाता नजर आ रहा है इससे उपभोक्ता की हालत में कोई सुधार नही हो रहा है बल्कि जब उत्पादक को कर राहत दी जाती है तो उससे सरकारी कोष को ही नुकसान पहुंचता है क्योंकि सरकार को मिलने वाले राजस्व में कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिये आम आदमी की जमा पूंजी पर ब्याज दरें कम कर दी जाती है 2014 से ऐसा लगातार हो रहा है। हर आदमी को ब्याज दरें घटने से नुकसान हुआ है। राजनीतिक दल इस पर खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि विरोध के हर स्वर को देशद्रोह करार दिया जा रहा है। जब इकबाल की प्रार्थना मदरसे में गाये जाने पर सज़ा दी जा सकती है तो फिर उससे आगे कुछ भी बोलने को शेष नहीं रह जाता है। आज राजनीतिक दलों से ज्यादा तो आम आदमी की सहन शक्ति परीक्षा की कसौटी पर आ गयी है। क्योंकि जब आम आदमी की बैंकों में रखी जमा पंूजी पर असुरक्षा की तलवार लटक जाती है तब उसके पास व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। न्यायपालिका जब सरकार के खिलाफ यह टिप्पणी करने लग जाये कि वहां पर कानून और व्यवस्था की जगह अराजकता ने ले ली है तब आम आदमी का विश्वास का अन्तिम सहारा भी चूर चूर हो जाता है। आज दुर्भाग्य से देश उसी स्थिति की ओर धकेला जा रहा है जो आजादी से पहले थी तब भी देश की पंूजी कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित थी और आज भी वैसा ही होने जा रहा है।
विपक्ष अभी भी हताशा में क्यों
- Details
- Created on Monday, 14 October 2019 13:53
- Written by Shail Samachar


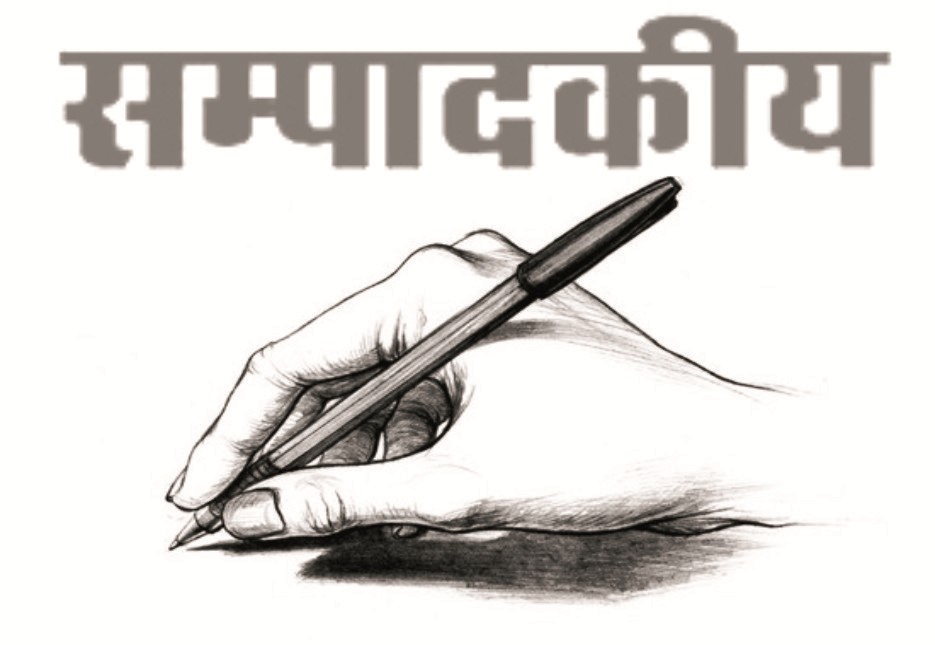
‘‘ऐसे मुद्दे जो प्रभावित तो सबको करें परन्तु सबकी समझ न आ सके’’ जब समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तब राजनीतिक दलों की आवश्यकता और उनकी भूमिका महत्वूपर्ण हो जाती है। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आम आदमी को उसी के हाल पर छोड़ देने से काम नही चलता। ऐसी वस्तुस्थिति में पूरी निष्पक्षता के साथ यह आकलन करना पड़ता है कि जो घट रहा है वह कहीं नीतियों की कुटिलता का परिणाम है या नीतियों में ना समझी का प्रतिफल है। क्योंकि नासमझी को तो समझ से दूर किया जा सकता है। जबकि कुटिलता पूरी समझ के साथ, नीयत के साथ की जाती है। ऐसी कुटिलता को जायज ठहराने के लिये साम, दाम, दण्ड और भेद जैसी सारी चाले चली जाती हैं। इस कुटिलता और नासमझी में विवेक करना ही राजनीतिक दलों का धर्म और कर्तव्य है। लेकिन आज विपक्ष इस मानदण्ड पर खरे नही उतर रहे हैं। बल्कि पूरी तरह विमुखनजर आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वभाविक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर ही हताश या निराश हो गया है या उसमें वैचारिक विश्लेषण का संकट आ खड़ा हुआ है। इस संद्धर्भ में यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले ही देश को कांग्रेस मुक्त करने का लक्ष्य घोषित कर दिया था जो शायद 2019 के चुनावों के बाद विपक्ष मुक्त भारत बन गया है। देश कांग्रेस मुक्त हो जाये या विपक्ष मुक्त यह इतना महत्वपूर्ण नही है इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसमें आम आदमी कहां खड़ा होगा।
इस समय मंहगाई का आलम यह है कि जिस प्याज को लेकर कभी नरेन्द्र मोदी ने ही यह तंज कसा था कि अब प्याज को तिजोरी में रखना पड़ेगा आज वही प्याज उन आंकड़ों से भी आगे निकल गया है लेकिन कहीं से कोई संगठित विरोध सामने नही आ रहा है। जिस व्यवस्था में भीड़ हिंसा पर सवाल उठाने के लिये अदालत सवाल उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे वहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब देश के कानून मंत्री आर्थिक मंदी को फिल्म की कमाई के तराजू पर तोलने लगे तो उसकी मानसिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। जहां विरोध को दबाने के लिये ईडी और सीबीआई जैसी ऐजैन्सीयों का खुलकर उपयोग होने लगे वहां के हालात को समझना आम आदमी के बस की बात नही रह जाती है। सत्ता पक्ष के पास एक विचारधारा है यह विचारधारा भारत जैसे बहुविध समाज के लिये कितनी हितकर हो सकती है? विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश में निजि क्षेत्र के हवाले ही सब कुछ छोड़ देना कितना हितकर हो सकता है। इन सवालों पर आज साहस पूर्ण सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है लेकिन यह बहस अंबानी और अदानी के खरीदे हुए चैनलों के मंच से संभव नही है। इसके लिये कांग्रेस जैसे बड़े दल को ही आगे आना होगा। कांग्रेस और उसके नेतृत्व को यह तय करना होगा कि उसके पास खुली लड़ाई लड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नही रह गया है। इस लड़ाई के लिये एक बार फिर गांधी और नेहरू की वैचारिक विरासत को विस्तार देना होगा। कांग्रेस जनो और आम आदमी को यह समझना होगा कि नेहरू और डाक्टर प्रशांत चन्द्र महाल नोबिस ने विकास की जो परिकल्पना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की थी आज भी वही अवधारणा प्रसांगिक है इस अवधारणा का मूल गांधी की विचारधारा थी कि जिस देश में मैन पावर जितनी अधिक होती है उसका मशीनीकरण बहुत सोच समझकर करना होता है। लाभ की अवधारणा पर आधारित विकास कालान्तर में समाज के लिये घातक होता है यह एक स्थापति सत्य है।
मोदी की अमरीका यात्रा के बाद दवाईयों की कीमतों मे बढौतरी क्यों
- Details
- Created on Monday, 30 September 2019 12:20
- Written by Shail Samachar

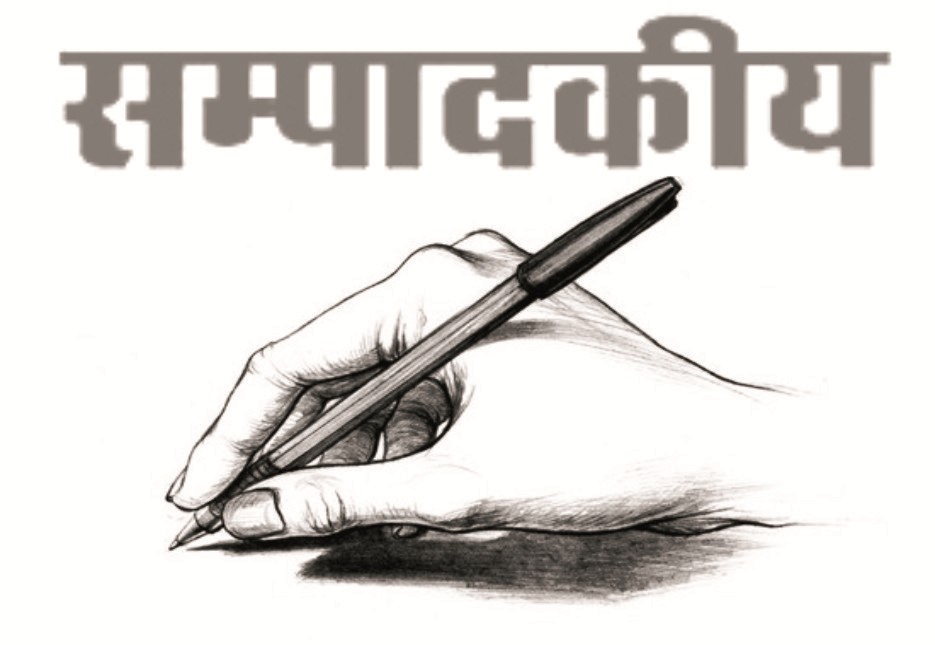
प्रधानमन्त्री की अमरीका यात्रा और यूएन में उनके भाषण के बाद कुछ चैनलों ने मोदी जी को विश्व विजेता और फादर आफ नेशन तक के संबोधन दिये हैं। इन चैनलों की राय ऐसी हो सकती है और उन्हे ऐसी राय रखने का अधिकार भी है। मैं उनके इस अधिकार पर कोई आपति नही उठा रहा हूं भले ही ओवैसी ने फादर आॅफ नेशन पर अपनी आपति दर्ज कराई है। मेरा यहां पर मोदी जी और उनके प्रशंसक चैनलों से इतना ही आग्रह है कि मोदी और ट्रंप की घनिष्ठ दोस्ती सबके सामने आ चुकी है। यदि इस दोस्ती के लाभ के रूप में ट्रंप भारतीय निर्यात पर लगाये गये उस शुल्क को वापिस ले लेते जिसके कारण देश के व्यापार को 38000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा हैं मैं यह आग्रह इस आधार पर कर रहा हूं कि जब मोदी जी ट्रंप के लिये ‘‘अब की बार ट्रंप सरकार ’’ का वातावरण बनाकर आये हैं और मोदी के इस नारे पर अमेरीकी भारतीयों ने भी अपनी मोहर लगा दी है तो बदले में देश को यह राहत तो मिलनी ही चाहिये थी। क्योंकि ऐसे अवसर बार-बार नही मिलते हैं और अब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है और उससे यह आशंका बढ़ भी गयी है।
मोदी जी ने इस यात्रा में यू एन को संबोधित करते हुए पूरे विश्व को यह बताया है कि भारत में सब कुछ अच्छा है। विश्व को यही बताया जाना चाहिये था। इमरान खान ने यू एन में अपने 50 मिनट का भाषण में कश्मीर को लेकर जो कुछ विश्व को बताया है उसका व्यवहारिक जवाब मोदी जी को अपने देश में अपने आचरण से देना होगा। कश्मीर के हालात क्या हैं उसके बारे में देशवासी अपने तौर पर जानते हैं। देशवासी जानते हैं कि प्रधानमन्त्री का यू एन संबोधन शेष विश्व के लिये था। देश जानता है कि कश्मीर में अभी तक भी प्रतिबन्ध यथास्थिति बने हुए हैं। वहां कालेज और विश्वविद्याालय अभी तक बन्द चल रहे हैं। अभी भी संचार सेवायें पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। फारूख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर गृहमन्त्री के संसद में ब्यान और बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद आये ब्यान में विरोधाभास खुल कर सामने आ चुका है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पर मसूद अहमद भट्ट को लेकर उसकी पत्नी की याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के जस्टिस अली मोहम्मद मैगरे के 25-9-19 को सुनाये फैसले से वहां प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। अदालत ने भट्ट की तुरन्त रिहाई के आदेश दिये हैं। दो नाबालिगों को भी इसी तरह बंदी बनाये जाने पर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब तलब किया है। ऐसे दर्जनों मामले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक आये हुए हैं। ऐसे मामलों को देर तक लंबित रखने से अदालत की साख पर भी प्रश्न चिन्ह लगने की स्थिति आ जायेगी। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के औचित्य को देश की जनता को समझाने के लिये पिछले दिनों संगठन की जिम्मेदारी लगाई थी और संगठन ने ऐसा हर राज्य में किया भी है। माना जा रहा है कि संगठन के इस प्रयास के बाद राज्य में हालात एकदम सामान्य हो जायेंगे और वहां से हर तरह के प्रतिबन्ध हटा लिये जायेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका है जिससे साफ हो जाता है कि इस सम्बन्ध में दिया जा रहा स्पष्टीकरण पूरी तरह लागों के गले नहीं उतर रहा है।
इस परिदृश्य मे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह सब कुछ कब तक ऐसे चलता रहेगा और इसका अन्तिम परिणाम क्या होगा। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर ई.डी. और सी.बी.आई. की सक्रियता कुछ विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर बढ़ती नज़र आ रही है उससे भी जनता में कोई अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। क्योंकि आजम खान के मामले में बकरी चोरी, किताब चोरी और पेड़ चोरी जैसे आरोप लगने से संवद्ध प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे हैं। चिन्मयानन्द के मामले में पीड़िता लड़की का जेल में होना इन्हीं सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाता है। इसलिये आवश्यक है कि सारे राजनैतिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर सारी वस्तुस्थिति पर समय रहते निष्पक्षता से विचार कर लिया जाये।
उत्पादक की क्षमता से पहले उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ानी होगी
- Details
- Created on Monday, 23 September 2019 06:20
- Written by Shail Samachar

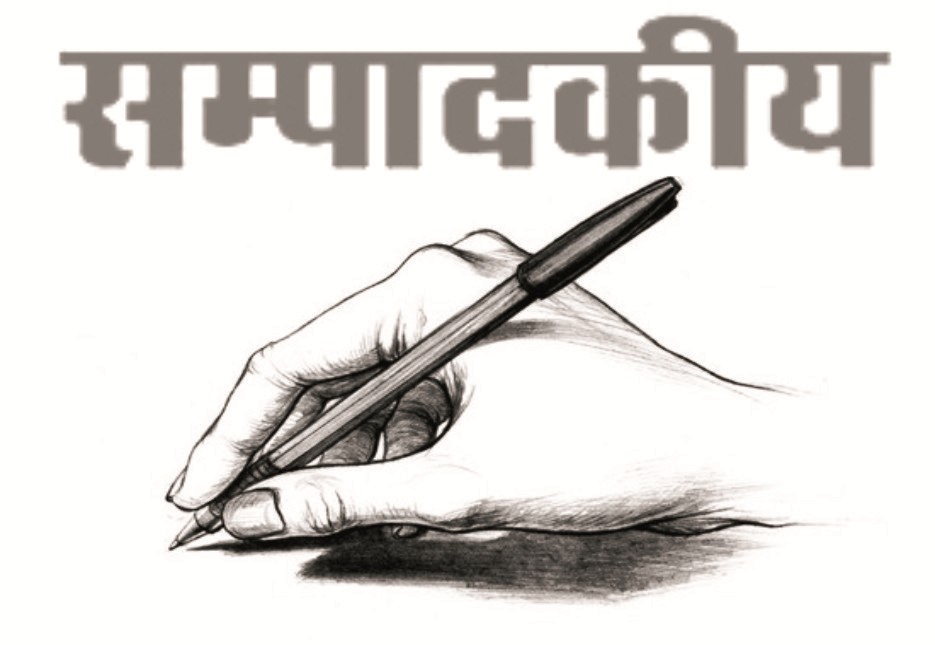
सरकार की 1.45 लाख करोड़ की राहत के साथ बाज़ार में खुशी की लहर देखने को मिली है। बाज़ार में निवेश में एकदम उछाल आया है। इस राहत से उत्पादन में जो कमी आयी थी वह रूक जायेगी उसमें बढ़ौत्तरी भी आ जायेगी और रोज़गार जाने का जो संकट पैदा हो गया था उसमें भी कुछ रोक लग जायेगी। मोटर गाड़ियां और हाऊसिंग का निर्माण फिर पुरानी चाल पर आ जायेगा यह माना जा रहा है। लेकिन इस सबसे खरीद पर भी असर पड़ेगा इसको लेकर संशय है। बाज़ार में 55 हजार करोड़ की गाड़ियां पहले से मौजूद हैं लेकिन उन्हे खरीदने वाला कोई नहीं था इसलिये आटोमोबाईल क्षेत्र में मंदी आयी थी। इसी तरह बाज़ार में 18 लाख घर बनकर तैयार हैं परन्तु लेने वाला कोई नही है। मंदी की तो परिभाषा ही यह है कि आपके पास बेचने के लिये तो सामान तैयार है परन्तु लेने वाला कोई नही हैं। इसका पता इसी से चल जाता है कि आरबीआई पांच बार ऋण की ब्याज दरों पर कटौती की घोषणाएं कर चुका है। यह घोषणाएं यह प्रमाणित करती है कि निवेशक और उपभोक्ता दोनो ही ऋण लेने से कतरा रहे हैं। क्योंकि दोनों के पास ऋण वापिस करने के पर्याप्त साधन नही हैं और बैंक भी एनपीए का और बोझ उठाने की स्थिति में नही हैं।
इस परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि आखिर यह हालात पैदा क्यों और कैसे हो गये? क्या सरकार की प्राथमिकताएं अव्यवहारिक हो गयी हैं। सरकार जब छोटे किसानों और दुकानदारों को पैन्शन तथा गरीबों को ईलाज के लिये आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं लाने की बात करती है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मानती है कि उसकी योजनाओं से समाज के इस वर्ग का जीवन यापन कठिन हो गया है। यह वर्ग सरकार की योजनाओं के गुण दोषों का आकलन करने न लग जाये इसलिये उसे इस तरह की राहतें देकर कुछ समय के लिये शांत रखने का उपाय किया गया है। लेकिन यहां यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कब तक किया जा सकता है। आज एक वर्ग को 1.45 लाख करोड़ की राहत देकर मंदी से बाहर निकालने का उपाय किया गया है लेकिन जिस ढंग से सरकारी निकायों का विनिवेश किया जा रहा है और सभी सरकारी उपक्रमों के 75% सरप्लस संसाधनों को समेकित निधि में शामिल करने के लिये आदेश किये जा चुके हैं क्या उससे आने वाले समय में यह सरकारी उपक्रम स्वतः ही बन्द होने की कगार पर नही आ जायेंगें तब बेरोज़गारों का एक और बड़ा वर्ग नहीं पैदा हो जायेगा? क्योंकि आज तो कोरपोरेट टैक्स घटाकर उद्योगपति को राहत दे दी गया है लेकिन उस राहत से उपभोक्ता की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है और जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उससे यह क्रय शक्ति भविष्य में भी बढ़ने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।
आम आदमी के पास आय के सामान्य संसाधन क्या रह गये हैं? आज भी देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और यह प्रमाणित सत्य है कि जब तक कृषि पर आत्मनिर्भरता नहीं बनेगी तब तक औद्यौगिक निर्भरता का कोई बड़ा अर्थ नहीं रह जाता है। कृषि पर आधारित किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता जा रहा है और उद्योगपत्ति हज़ारों करोड़ का एनपीए डकार कर भी सुरक्षित और सम्मानित घूम रहा है। नोटबंदी के पांच दिन बाद ही 63 अरबपतियों का 6000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया था। उसी दौरान की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरबपति बैंकों का आठ लाख करोड़ डकार गये थे और मोदी सरकार ने इसमें से 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिये थे। उस समय केजरीवाल ने वाकायदा एक पोस्टर के माध्यम से यह आरोप लगाये थे लेकिन आजतक इन आरोपों का कोई जवाब नही आया है। ऐसे ही कई और आरोप हैं जिनके जवाब नही आये हैं जिनमें कपिल सिब्बल का जाली नोटों को लेकर लगाया गया आरोप बहुत ही गंभीर है। आरोपों का जब सार्वजनिक रूप से जवाब नही आता है और न ही आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई कारवाई की जाती है तब आम आदमी के पास आरोपों को सच मानने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। आज सरकार इसी कगार पर पहुंचती जा रही है। इसलिये आर्थिक मंदी को रोकने के लिये उत्पादक से पहले उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। आर्थिकी एक ऐसा पक्ष है जिस पर हर आदमी अपनी-अपनी तरह चिन्ता और चिन्तन करता है क्योंकि भूखे आदमी के हर सवाल का जवाब केवल रोटी ही होता है।



