


ShareThis for Joomla!
क्या लोकतन्त्र बच पायेगा
- Details
- Created on Tuesday, 13 October 2020 12:49
- Written by Shail Samachar
 सर्वोच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे ज्यादा दुरूपयोग हुआ है शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी केन्द्र सरकार के उस स्टैण्ड पर की थी जिसमें कहा गया था कि तबलीगी जमात को लेकर दायर की गयी याचिकाएं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का गला घोंटने का प्रयास है। तबलीगी जमात का अधिवेशन दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में मार्च में हुआ था। इस अधिवेशन की समाप्ति के साथ ही लाकडाऊन लागू हो गया था। यातायात के सारे साधन बन्द हो गये और इसी कारण से यह लोग अपने-अपने घरों को वापिस नहीं जा पाये। जब वापिस नहीं जा पाये तो मरकज़ में इकट्ठे रहना पड़ा। इस तरह इकट्ठे रहना लाकडाऊन के नियमों का उल्लंघन बन गया। यह लोग मुस्लिम समुदाय से थे इसलिये इनके खिलाफ हर तरह का प्रचार शुरू हो गया। मीडिया ने कोरोना का कारण ही इन लोगों को बना दिया। कोरोना बम्ब की संज्ञा तक दे दी गयी। तबलीगी के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। पूरे समाज में मुस्लिम समुदाय को नफरत का पात्र बना दिया गया और यह काम किया मिडिया ने। मीडिया के इस नफरती प्रचार पर रोक लगाने के लिये शीर्ष अदालत में छः अप्रैल को ही एक याचिका दायर हो गयी। लेकिन तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रचार पर यह कहकर रोक लगाने से इन्कार कर दिया कि ऐसा करना प्रैस की आजा़दी का गला घोंटना होगा। परन्तु अब यह मामला सुनवाई के लिये आया तब केन्द्र सरकार ने भी इन याचिकाओं को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हमला करार दिया। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने केवल इस तर्क को खारिज ही किया बल्कि केन्द्र सरकार को गंभीर लताड़ भी लगायी। शीर्ष अदालत की यह लताड़ उस सबका परिणाम है जो 24 मार्च से लेकर अब तक कोरोना काल में घटा है। क्योंकि तबलीग को लेकर इस दौरान कुछ उच्च न्यायालयों ने जो फैसले दिये हैं उससे सारी धारणाएं ही बदल गयी हैं। हरेक ने इसे मीडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे ज्यादा दुरूपयोग हुआ है शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी केन्द्र सरकार के उस स्टैण्ड पर की थी जिसमें कहा गया था कि तबलीगी जमात को लेकर दायर की गयी याचिकाएं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का गला घोंटने का प्रयास है। तबलीगी जमात का अधिवेशन दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में मार्च में हुआ था। इस अधिवेशन की समाप्ति के साथ ही लाकडाऊन लागू हो गया था। यातायात के सारे साधन बन्द हो गये और इसी कारण से यह लोग अपने-अपने घरों को वापिस नहीं जा पाये। जब वापिस नहीं जा पाये तो मरकज़ में इकट्ठे रहना पड़ा। इस तरह इकट्ठे रहना लाकडाऊन के नियमों का उल्लंघन बन गया। यह लोग मुस्लिम समुदाय से थे इसलिये इनके खिलाफ हर तरह का प्रचार शुरू हो गया। मीडिया ने कोरोना का कारण ही इन लोगों को बना दिया। कोरोना बम्ब की संज्ञा तक दे दी गयी। तबलीगी के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। पूरे समाज में मुस्लिम समुदाय को नफरत का पात्र बना दिया गया और यह काम किया मिडिया ने। मीडिया के इस नफरती प्रचार पर रोक लगाने के लिये शीर्ष अदालत में छः अप्रैल को ही एक याचिका दायर हो गयी। लेकिन तब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रचार पर यह कहकर रोक लगाने से इन्कार कर दिया कि ऐसा करना प्रैस की आजा़दी का गला घोंटना होगा। परन्तु अब यह मामला सुनवाई के लिये आया तब केन्द्र सरकार ने भी इन याचिकाओं को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर हमला करार दिया। लेकिन अब शीर्ष अदालत ने केवल इस तर्क को खारिज ही किया बल्कि केन्द्र सरकार को गंभीर लताड़ भी लगायी। शीर्ष अदालत की यह लताड़ उस सबका परिणाम है जो 24 मार्च से लेकर अब तक कोरोना काल में घटा है। क्योंकि तबलीग को लेकर इस दौरान कुछ उच्च न्यायालयों ने जो फैसले दिये हैं उससे सारी धारणाएं ही बदल गयी हैं। हरेक ने इसे मीडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया है।
इसी दौरान फिल्म अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत की मौत का मामला आ गया। इस मौत को आत्महत्या की बजाये हत्या करार दिये जाने लगा इसके तार ड्रग माफिया से जुड़े होने के खुलासे होने लगे। देश की सारी जांच एजैन्सीयां इसी मामले की जांच मे लग गयी। ड्रग्ज़ के लिये कुछ लोगों की गिरफ्तारियां तक हो गयी। पूरे मामले को बिहार, महाराष्ट्र प्रौजैक्ट किया जाने लगा। अभिनेत्री कंगना रणौत ने तो यहां तक कह दिया कि यह हत्या का मामला है और इसके सबूत उसके पास हैं। यदि वह अपने आरोपों को प्रमाणित नही कर पायेंगी तो पद्मश्री लौटा देंगी। न्यूज चैनलों से अन्य सारे मुद्दे गायब हो गये। केवल सुशान्त सिंह राजपूत और कंगना रणौत ही प्रमुख मुद्दे बन गये। केन्द्र ने कंगना को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान कर दी। हिमाचल भाजपा ने तो कंगना के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान प्रदेशभर में छेड़ दिया। लेकिन इसी बीच जब एम्ज़ की विशेषज्ञ कमेटी ने सुशान्त सिंह की मौत को हत्या की बजाये आत्महत्या करार दिया तब इस मामले का भी पूरा परिदृश्य ही बदल गया। इस बदलाव पर एनबीएसए भी गंभीर हुआ। उसने आजतक, एबीपी इण्डिया टीवी और न्यूज 18 जैसे कई चैनलों को सुशान्त राजपूत केस में गलत जानकारीयां देने तथ्यों को छुपाने और तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसे कई गंभीर आरोपों का दोषी पाते हुए कुछेक को एक-एक लाख तक का जुर्माना लगाया है। एनबीएसए न्यूज चैनलों का अपना एक शिखर संगठन है। इस संगठन द्वारा भी इन चैनलो को देाषी करार देना अपने में ही मीडिया की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। फिर इसी बीच मुंबई पुलिस न्यूज चैनलों के टीआरपी घोटाले का अनाचरण कर देती है इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। रिपब्लिक टीवी को भी इस प्रकरण में नोटिस जारी किया गया है। इस तरह मीडिया के इन सारे मामलों को अगर इकट्ठा करके देखा जाये तो निश्चित रूप से यह बड़ा सवाल जवाब मांगता है कि क्या इस चैथे खम्बे के सहारे लोकतन्त्र कितनी देर खड़ा रह पायेगा?
मीडिया पर उठी यह बहस अभी शुरू ही हुई है कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री जगन रेड्डी ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को एक छः पन्नो का पत्र भेजकर शीर्ष अदालत के ही दूसरे वरिष्ठतम जज रम्मन्ना के खिलाफ आरोप लगाकर लोकतन्त्र के एक और खम्बे न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया है। जगन रेड्डी स्वयं आपराधिक मामले झेल रहे हैं और जस्टिस रम्मन्ना ने ही माननीयों के खिलाफ देशभर में चल रहे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के आदेश पारित किये हैं। ऐसे में रेड्डी में इस पत्र को न्यायपालिका बनाम व्यवस्थापिका में एक बड़े संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। क्योंकि रेड्डी स्वयं मुख्यमन्त्री हैं और उनके कहने लिखने का भी एक अर्थ है। दिल्ली उच्च न्यायालय के भी एक जज के खिलाफ पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह, आनन्द चैहान के माध्यम से ऐसे ही आरोप एक समय लगा चुके है। तब इसकी ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित नही हुआ था और आज यह पत्र संस्कृति सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक दे चुकी है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तो बहुत अरसा पहले ही जन विश्वास खो चुकी है और अब मीडिया तथा न्यायपालिका की अस्मिता भी सवालों के घेरे में आ खड़ी है। ऐसे में यदि समय रहते लोकतन्त्र के इन खम्बों पर उठते सवालों के जवाब न तलाशे गये तो यह तय है कि लोकतन्त्र नहीं बच पायेगा।
निर्भया-गुड़िया और हाथरस कब तक घटते रहेंगे
- Details
- Created on Tuesday, 06 October 2020 12:05
- Written by Shail Samachar




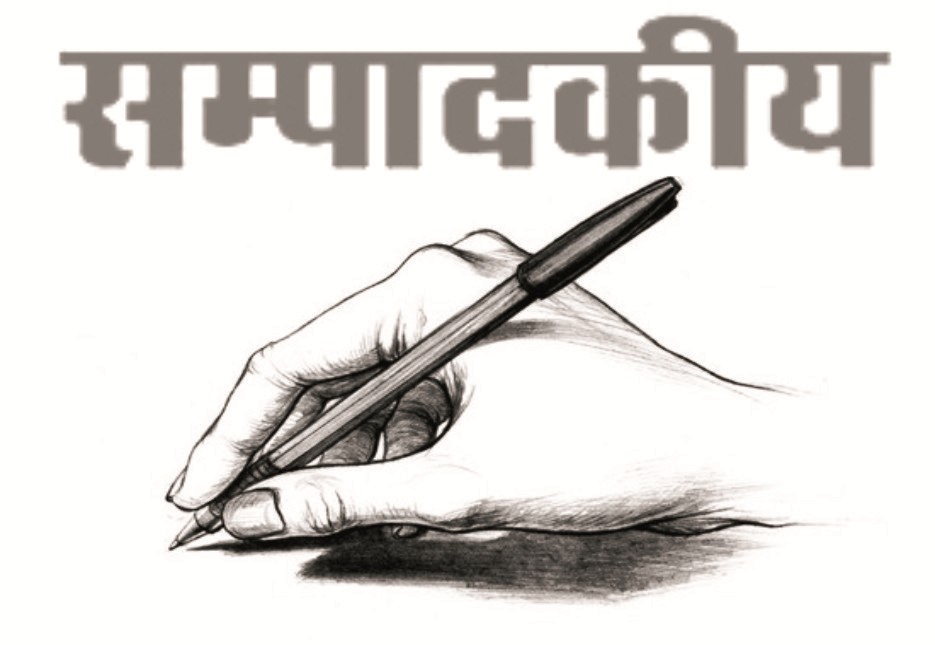
पूर्व में जब निर्भया कांड दिल्ली में घटा और फिर हिमाचल में गुड़िया प्रकरण हुआ तब भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। इन सवालों से सरकारें भी सवालों के घेरे में आ गयी थी। आज हाथरस प्रकरण में फिर पुलिस और सरकार अविश्वास के आरोपों में घिरी हुई है। इससे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि आखिर पुलिस पर से विश्वास क्यों उठता जा रहा है। फिर दूसरा सवाल उठता है कि यह अपराध क्यों बढता जा रहा है। आज शायद देश का कोई राज्य ऐसा नही बचा है जहां पर गैंगरेप और फिर हत्या के कांड न हुए हो। अभी हाथरस का आक्रोश थमा भी नही था कि उत्तरप्रदेश के ही बुलन्दरशहर में एक दलित लड़की के साथ ऐसा ही काण्ड घट गया। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में गुड़िया काण्ड के बाद अब तक गैंगरेप के 43 मामले घट गये हैं। गैंगरेप के बाद हत्याएं भी हुई हैं। जिस तरह से यौन अपराधों का आंकड़ा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है उससे यह सवाल उठता है कि क्या समाज ही मानसिक रूप से बीमार हो गया है? क्या आम आदमी को पुलिस और सज़ा का डर ही नहीं रह गया है? क्या जब किसी मामले पर किन्हीं कारणों से जनाक्रोश उभरेगा तब उस पर न्याय की मांग भी उठेगी और कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ कारवाई भी हो जायेगी? सत्ता तक भी बदल जायेगी और उसके बाद ‘ढाक के वही तीन पात’ घटते रहेंगे?
मैं यह आशंका हिमाचल की ही व्यवहारिक स्थिति को सामने रखकर उठा रहा हंू। 2017 मई में प्रदेश में गुड़िया कांड घटा। भाजपा विपक्ष में थी। पुलिस इस मामले की अभी प्रारम्भिक जांच ही शुरू कर पायी थी कि इसमें मीडिया रिपोर्ट आनी शुरू हो गयी। पुलिस पर शक शुरू हो गया और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने दखल दिया और जांच सीबीआई को सौंप दी गयी। प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक गुड़िया को न्याय दिलाने के लिये कैण्डल मार्च हुए। सबकुछ हुआ जो आज हाथरस में देखने को मिला है। दिसम्बर में प्रदेश के चुनाव थे यह गुड़िया एक बड़ा मुद्दा बना और सत्ता बदल गयी। लेकिन गुड़िया को अभी तक न्याय नहीं मिला है। बल्कि गुड़िया काण्ड के बाद गैंगरेप के 43 मामले और बढ़ गये। जिनमें कांगड़ा के फतेहपुर में दलित लडक़ी की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला है लेकिन इस मामले में कोई बड़ी प्रभावी कारवाई अभी तक नही हुई है। भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस ने विधानसभा में बलात्कारों तथा गैंगरेपों पर सवाल पूछकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। विधानसभा मे यह सवाल चर्चा में आ ही नहीं पाया केवल लिखित उत्तर तक ही रह गया। इससे सबकेे सरोकारों का अन्दाजा लगाया जा सकता है।
इस परिपे्रक्ष में यह तलाशना महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है कि आखिर यह अपराध बढ़ क्यों रहा है? कानून और न्याय का डर तो खत्म होता जा रहा है? इन सवालों पर मंथन करते हुए सबसे पहले तो यह सामने आता है कि आज संसद से लेकर विधानसभाओं तक दर्जनों माननीय ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, अपराध और बलात्कार के मामले दर्ज हैं और वर्षों से लंबित चल रहे हैं। मोदी जी ने भी यह वायदा किया था कि वह संसद को अपराधियों से मुक्त करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कदम इस दिशा में उठा नहीं पाये हैं। सरकार के बाद दूसरी उम्मीद न्यायपालिका से होती है। लेकिन जब देश के प्रधान न्यायधीश के खिलाफ ही ऐसी शिकायत आई तब जांच के लिये जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गयी उससे यह सामने आ गया कि कानून आम आदमी और विशेष आदमी के लिये कैसे अलग-अलग हो जाता है। न्यायपालिका के बाद मीडिया आता है, उम्मीद की जाती है कि मीडिया जनहित में इसके खिलाफ जिहाद करेगा। लेकिन वहां भी जब ‘‘मीटू’’ के आरोप सामने आ गये और मीडिया पीड़ित को छोड़कर पुलिस और सरकार के साथ खड़ा होकर आक्रोशितों के सामने विभिन्न राज्यों के आंकड़े उछालते हुए जनाक्रोश को कुन्द करने के प्रयासों में लग जाये तो वहां से भी कोई उम्मीद करना बेनामी हो जाता है। ऐसे में अन्त में यही बच जाता है कि आम आदमी के स्वयं ही लामबन्द्ध होकर यह आन्दोलन करना होगा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानून की प्रक्रिया एक जैसी ही रहे। ऐसे आरोप झेल रहे माननीयों की संसद/विधानसभा की सदस्यता तुरन्त प्रभाव से खत्म करते हुए यह सुनिश्चित किया कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ अपहरण-बलात्कार ,हत्या के आरोप लगे हों उसे तब तक चुनाव न लड़ने दिया जाये जब तक वह दोष मुक्त न हो जाये। संसद में इस आश्य का कानून पारित किये जाने की मांग की जानी चाहिये। इसी के साथ सोशल मीडिया के मंचो पर भी कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि इस समय दर्जनों साईटस ऐसी आप्रेट कर रही हैं जो यौनाचार को व्यवसाय की तरह परोस और प्रमोट कर रही हैंैै। इनके विडियो मोबाईल फोन पर उपलब्ध रहते हैं और इसका प्रभाव/परिणाम इस तरह के अपराधों के रूप में सामने आ रहा है। यदि सोशल मीडिया में बढ़ते इस तरह के पोस्टो पर ही प्रतिबन्ध लगा रहे हों तो निश्चित रूप से इन अपराधों में कभी आयेगी।
सरकार जल्दबाजी में क्यों क्या कोई बड़ा ऐजैण्डा आने वाला है
- Details
- Created on Tuesday, 29 September 2020 06:47
- Written by Shail Samachar

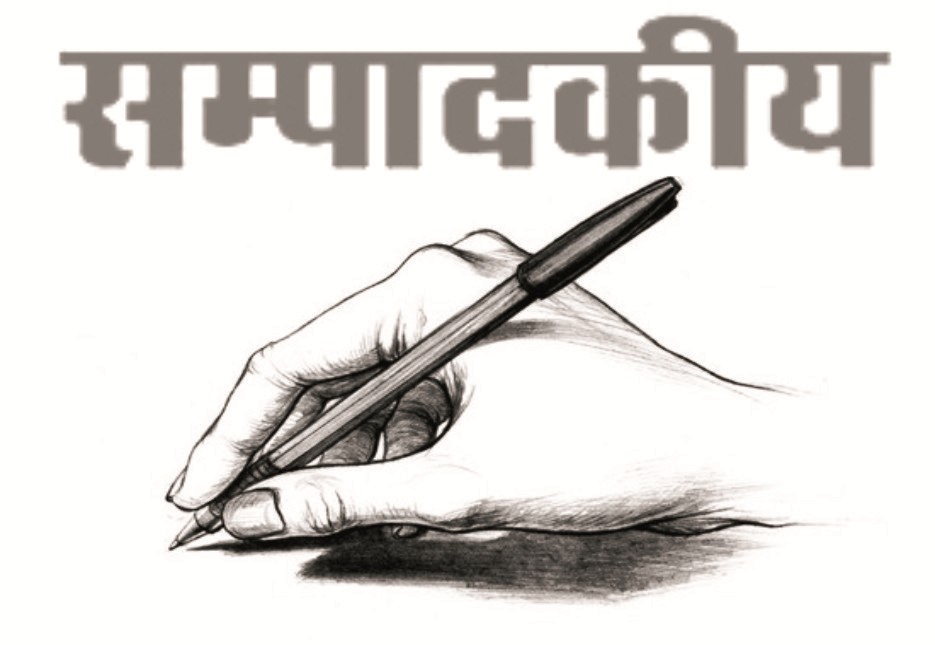
इस समय देश कोरोना के संकट से लड़ रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। करोड़ो लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हर आदमी प्रभावित हुआ है और कुछ भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। सरकार भी इस स्थिति को जानती है इसलिये तो आर्थिक पैकेज जारी किया गया था। ऐसे मे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब सरकार जानती है कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है तब भी इस तरह के विधेयक लाकर इस संकट को और क्यों बढ़ाया जा रहा है? फिर संसद में और संसद से बाहर इन पर कोई चर्चा नहीं होने दी जाती है। जब भी किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर कोई सवाल उठाया जाता है तब उसे एकदम पहले प्रधानमंत्री स्व. नेहरू के काल तक ले जाते हुए मोदी से पहले तक के हर प्रधानमंत्री को दोषी ठहरा दिया जाता है। पीएम फण्ड केयर को लेकर पुछे गये सवाल में संसद में यह सब देखने को मिल चुका है। इससे यह आशंका उभरती है कि सरकार जान बुझकर एक अराजकता जैसा वातावरण खड़ा कर रही है। ऐसा लगता है कि अराजकता के माहौल में किसी और बड़े ऐजैण्डे पर काम किया जा रहा है। क्योंकि इस समय संसद में जो बहुमत हासिल है वैसा दोबारा मिलना कठिन है। हर ऐजैण्डे के लिये संसद के ही मार्ग से होकर आना होगा। शीर्ष न्यायपालिका और बड़े मीडिया से इस समय विरोध आने की कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। आम आदमी महामारी से डरा हुआ है। इस तरह का वातावरण कुछ भी नया थोपने के लिये सबसे सही वक्त माना जाता है।
इस तरह की आशंकाएं इसलिये उभर रही हैं क्योंकि पिछले दिनो भाजपा नेता डा. स्वामी का जनवरी 2000 में फ्रन्टलाईन में छपा एक लेख अचानक चर्चा में आ गया है। इस लेख में डा. स्वामी ने आरएसएस की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए खुलासा किया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अक्तूबर 1998 मे हुए अधिवेशन में वर्तमान संसदीय प्रणाली को बदलने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें दो सदनों के स्थान पर तीन सदन बनाने की बात की गयी है। इस लेख की चर्चा सामने आते ही भाजपा के मीडिया सैल ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। डा. स्वामी ने जवाबी हमला करते हुए आईटी सैल के प्रमुख अमित मालवीय को ही हटाने की मांग कर दी थी। भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से इस प्रसंग का कोई खण्डन नही आया है। स्वामी के इस लेख के बाद संघ के नेता राजेश्वर सिंह का ब्यान सामने आता है। इन्होंने मोदी के प्रधानमन्त्री बनने के बाद कहा था कि ‘‘हमारा लक्ष्य भारत को 2021 तक हिन्दुराष्ट्र बनाना है...’’ इसके लिये संस्कार भारती के साथ आरोग्य भारती ईकाईयों द्वारा उत्तम सन्तति के लिये गर्भ विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रों की 2020 तक प्रत्येक राज्य में स्थापना की योजना का जिक्र किया गया है। गुजरात के जामनगर, गांधी नगर और अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय भोपाल में गर्भ विज्ञान संस्कार पाठ्यक्रम शुरू हो चुकने का दावा किया गया है। देश के कई शहरों में इस आश्य के सैमीनार आयेजित हो चुके हैं। हिन्दु राष्ट्र के लिये संघ की कार्य योजना किस तरह की है इसकी विस्तृत चर्चा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रो. शमशुल ईस्लाम के एक आकलन से सामने आयी है। इसका भी कोई खण्डन नही आया है। हिन्दु राष्ट्र के इस ऐजैण्डे को असम उच्च न्यायालय के न्यायधीश जस्टिस चैटर्जी के उस फैसले से और बल मिल जाता है जिसमें उन्होंने स्वतः संज्ञान में ली एक याचिका पर यह फैसला दिया है कि भारत को अब हिन्दुराष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिये और मोदी जी में ही ऐसा करने की क्षमता है। इस फैसले के बाद डा. मोहन भागवत के नाम से भारत के नये संविधान की चर्चा भी बाहर आ चुकी है। इस प्रस्तावित संविधान का प्रारूप शैल पाठकों के सामने बहुत पहले रख चुका है। इस प्रस्तावित संविधान के प्रकरण पर भी कोई खण्डन नही आया है।
इस तरह हिन्दुराष्ट्र के ऐजैण्डे की चर्चाएं पिछले कुछ समय से उठती आ रही है। इन चर्चाओं का कोई भी खण्डन न तो केन्द्र सरकार की ओर से और न ही आरएसएस की ओर से आया है। यदि समय समय पर उठी चर्चाओं को इकट्ठा मिलाकर देखा जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके माध्यम से देश की नब्ज देखी जा रही थी। इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि सरकार का अगला ऐजैण्डा निश्चित रूप से हिन्दुराष्ट्र होने जा रहा है।
प्रधानमन्त्री पर अविश्वास है कृषि विधेयकों पर उठा विरोध
- Details
- Created on Monday, 21 September 2020 17:59
- Written by Shail Samachar




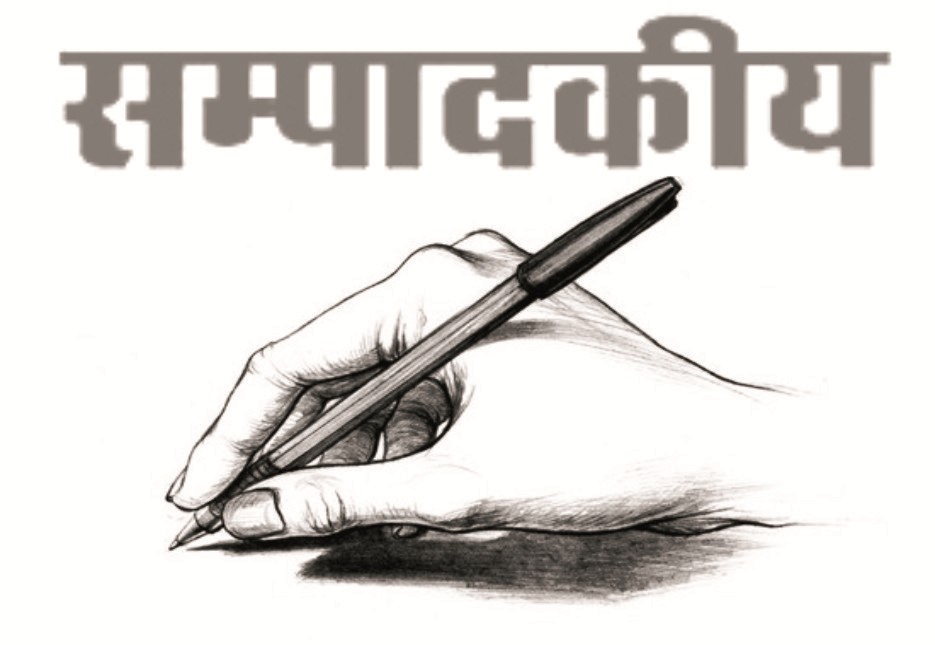
प्रधानमन्त्री से लेकर पूरी सरकार किसान विरोध को नाजायज़ बता रहे हैं। बल्कि यह पहली बार हो रहा है कि आम आदमी प्रधानमन्त्री और उनकी सरकार के किसी भी आश्वासन पर विश्वास करने को तैयार नही है। जिस जनता ने प्रधानमन्त्री पर आंख बन्द करके दो बार देश की सत्ता उनके हाथों में सौंप दी आज भी जनता उन पर विश्वास करने को तैयार नही है। इस स्थिति को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। 2014 में देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी थी। आज छः वर्षों के मोदी शासन पर नज़र डाले तो इस दौरान नोटबंदी और जीएसटी दो ऐसे सीधे आर्थिक फैसले रहे हैं जिन्होने आज जीडीपी को शून्य से भी नीचे पहुंचाने में पूरी भूमिका अदा की है। लेकिन इन फैसलों से आम आदमी सीधे प्रभावित नही होता था। इसलिये वह इनके विरोध का मन नही बना पाया। हालांकि 2014 से लेकर आज 2020 तक का एक बड़ा कड़वा सच यह भी रहा है कि आम आदमी के बैंकों में हर तरह के छोटे-बड़े जमा पर ब्याज दरें कम हुई हैं बैंको में आम आदमी के जमा पैसे की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। अभी करीब दो लाख करोड़ के बैंक फ्राड होने की जानकारी आरटीआई के माध्यम से बाहर आ चुकी है। जीरो बैलैन्स के नाम पर खोले गये जनधन खातों पर मिनिमम बैलैन्स की शर्त लग चुकी है। रसोई गैस पर सब्सिडी कम हो गयी है। उज्जवला योजना में अब मुुफ्त सिलैण्डर मिलना बन्द हो गया है। लेकिन इन सारे फैसलों का एक साथ आकलन करके उनका विरोध करने का मन आम आदमी नही बना पाया। शायद उसको लगा कि इन आर्थिक फैसलों से राम मन्दिर का निमार्ण, तीन तलाक समाप्त करना और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे तीन प्रदेशों में बांटना ज्यादा जरूरी फैसले थे।
इसी परिदृश्य के चलते चलते देश कोरोना के संकट का शिकार हो गया। एकदम बिना किसी पूर्व सूचना के सारे देश को घरों में लाॅकडाऊन के नाम पर बन्दी बना दिया गया। सारी आर्थिक गतिविधियों पर विराम लगा दिया गया। जून में अनलाॅक शुरू हुआ और उसमें पहला बड़ा फैसला आया कि सरकार ने 1955 से चले आवश्यक वस्तु अधिनियम को संशोधित करके अनाज, दल तिहन खाद्य तेल और आलू प्याज को इसके दायरे से बाहर कर दिया। यह वह चीजे़ हैं जो हर घर की रसोई की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार इनकी कीमतों और होर्डिंग पर नियन्त्राण रखती थी। इस संशोधन से यह चीजे सरकार के नियन्त्रण से बाहर हो गयी। लेकिन आम आदमी के सामने इसी के साथ (किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा तथा मूल्य आश्वासान और कृषि सेवा किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते ) नाम से दो और विधेयक जनता के सामने रख दिये। इस आश्य के अध्यादेश पांच जून को जारी किये गये थे। शैल के आठ जून के संपादकीय में इसकी संभावित आशंकाओं पर विस्तृत चर्चा की हुई है और आज वही आशंकाएं जन चर्चा में है। आज प्रधानमन्त्री कह रहे हैं कि इससे किसान बागवान को पूरा देश एक खुली मण्डी के रूप में हो जायेगा। किसान का जो उत्पीड़न आढ़ती के हाथों होता था उससे मुक्ति मिल जायेगी कृषि उत्पादों के व्यापार पर लगाने वाली सारी बंदिश समाप्त कर दी गयी है। उपज की खरीदारों का दायरा बढ़ जायेगा। बड़ी-बड़ी कंपनीयों के साथ वह खरीद और उत्पादन के समझौते कर पायेगा। यदि किसान को उसकी उपज का सही दाम नही मिल पाता है तो वह उसका भण्डारण कर सकता है। इसी साथ यह आश्वासन दिया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था भी जारी रहेगी।
यदि सरकार के इन सारे आश्वासनों का आकलन किया जाये तो इन सारे संशोधनों का मूल है कि किसान को उसकी उपज की उसकी लागत के अनुरूप कीमत मिले। लेकिन यह सुनिश्चित करने का कोई तन्त्रा नही रखा गया है। यह किसान और खरीदार के बीच सीधे संबंध पर आधारित होगा। लेकिन जिस भी व्यक्ति को किसानी और खेत का थोड़ा भी जाना ही संभव नही हो पाता है तो वह कहां कहां भटकता फिरेगा। क्या किसान के पास भण्डारण की सुविधा है शायद नही। ऐसे में क्या वह अन्तः में आढ़ती, अन्य व्यापारी या कंपनी की ही शर्तो पर उपज बेचने को बाध्य नही हो जायेगा। यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखती है तो क्या उससे किसान को उपज की मनमुताबिक कीमत मिल पायेगी? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य और मन मुताबिक कीमत आपस में स्वतः विरोधी नही है। क्या खुला बाज़ार बताकर सरकार स्वयं ही उत्पीड़न की श्रेणी में नही आ जायेगी क्योंकि वह तो न्यूनतम मूल्य देगी। फिर यदि न्यूनतम मूल्य जारी ही रखना है तो एक उपज एक बाजार और मनचाही कीमत का क्या अर्थ रह जायेगा। शायद आज किसान सरकार की कथनी और करनी के भेद को समझ चुका है। इसीलिये वह प्रधानमन्त्री पर भी विश्वास करने को तैयार नही है। उसे लग रहा है कि इन विधेयकों के माध्यम से उसे बहुराष्ट्रीय कंपनीयों के पास बन्धक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
भाजपा की पटकथा पर कंगना का अभिनय
- Details
- Created on Monday, 14 September 2020 18:33
- Written by Shail Samachar




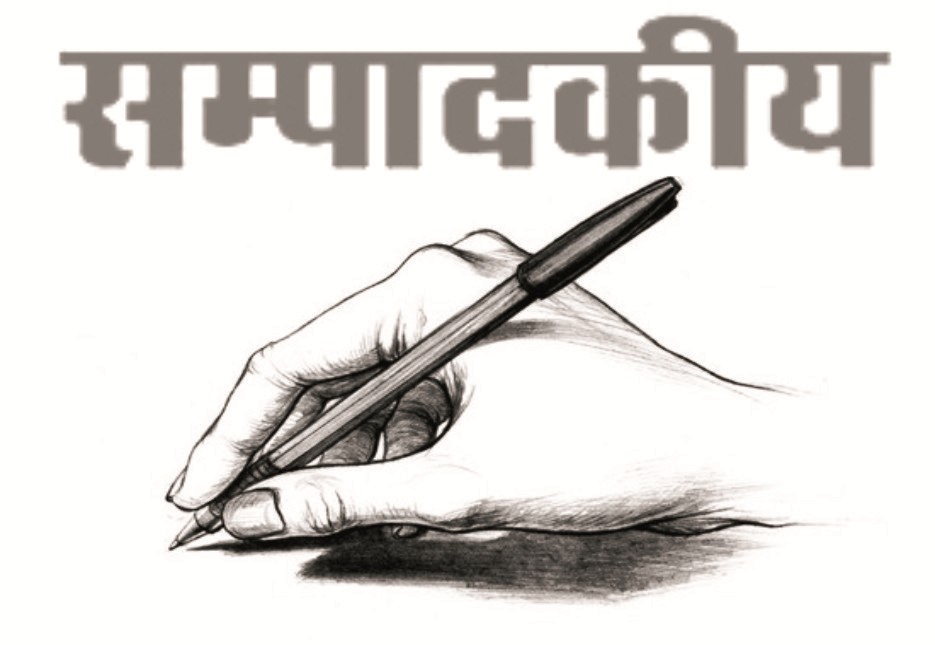
इस परिदृश्य में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कंगना-शिव सेना विवाद है क्या और क्यों शुरू हुआ। सिने अभिनेता स्व. सुशान्त सिंह राजपूत की मौत के बाद यह विवाद खड़ा हुआ कि आत्म हत्या ही है या हत्या है। यह सवाल इतना उलझ गया है कि चलते-चलते बिहार बनाम महाराष्ट्र राज्य पुलिस बनाम सीबीआई तक हो गया। ड्रग्स का सवाल इससे जुड़ गया है। ड्रग्स को लेकर पहला संकेत भापजा नेता डा.स्वामी के ब्यान से उभरा। आज इस मामले की जांच में केन्द्र की अलग-अलग ऐजैन्सीयों के दर्जनों अधिकारी उलझे हुए हैं और अभी तक यह मामला हल नही हो पाया है। यह माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनावों में भी यह मुद्दा बनेगा। इस सुशान्त प्रकरण में उस समय और गंभीरता बढ़ गयी जब इस मामले में हिमाचल की बेटी पदमश्री कंगना रणौत का अर्णब गोस्वामी के टीवी चैनल रिपब्लिक को दिया साक्षात्कार सामने आया। 19 जुलाई के इस साक्षात्कार में कंगना रणौत ने सुशान्त सिंह राजपूत की आत्म हत्या को एक सुनियोजित हत्या करार दिया। कंगना ने पूरे दावे के साथ सुशान्त की मौत को हत्या करार दिया और यहां तक कह दिया कि यदि वह इस आरोप को प्रमाणित नही कर पायेगी तो वह अपने पदमश्री सम्मान को वापिस कर देंगी।
कंगना ने इस साक्षात्कार में फिल्म जगत पर गंभीर आरोप लगाये हैं। पूरे दावे के साथ सिने जगत में मूवी माफिया के आप्रेट करने के आरोप लगाते हुए कई बड़े नामों का सीधे जिक्र किया है। आत्म हत्या तक के लिये उकसाने के आरोप कुछ लोगों पर लगाये हैं। इन्हीं आरोपों में कुछ तो सत्तारूढ़ शिव सेना को सीधे आहत करते हैं। इन आरोपों पर हर तरह की प्रतिक्रियाएं आना स्वभाविक था और आयीं। अर्णब गोस्वामी को दिये साक्षात्कार के बाद कंगना और शिव सेना में वाकयुद्ध शुरू हो गया। कंगना ने जब पूरे दावे के साथ यह कहा कि सुशान्त की हत्या की गयी है और वह उसे प्रमाणित कर सकती है। तब यह स्वभाविक और आवश्यक हो जाता है कि इस मामले की जांच कर रही एजैन्सीयां कंगना का ब्यान दर्ज करती। उसके दावों की पड़ताल की जाती। कंगना को इस संद्धर्भ में अपना ब्यान दर्ज करवाने के लिये बुलाया गया था लेकिन मनाली में होने के कारण वह नही गयी। जब कंगना ने सुशान्त की मौत को लेकर इतना बड़ा खुलासा कर दिया था और डा. स्वामी जैसा बड़ा भाजपा नेता इस प्रकरण में ड्रग्स माफिया की भूमिका की ओर संकेत कर चुका था तब शासन-प्रशासन की हर आॅंख का खुलना भी स्वभाविक हो जाता है। संभवतः इसी परिप्रेक्ष में बीएमसी भी सक्रिय हुई और कंगना के कार्यालय में हुए अवैध निर्माण पर दो वर्ष पहले दिये गये नोटिस पर सक्रिय हुई। इसी सक्रियता में अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। जब तोड़ फोड़ की कारवाई चल रही थी उस समय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। इस पर उच्च न्यायालय ने स्टे आदेशित करते हुए यथा स्थिति बनाए रखने को कहा है। लेकिन स्टे आदेशित होने से पहले ही तोड़ फोड़ पूरी हो चुकी थी। बल्कि उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि यह अवैधताएं एक रात में खड़ी नही हो गयी हैं। कंगना के निर्माणों में अवैधता है इससे कंगना ने इन्कार नही किया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इसे तोड़ने के लिये कंगना का वहां होना आवश्यक था? क्या कंगना जैसी पदमश्री से सम्मानित अभिनेत्राी को ऐसी अवैधताओं की वकालत करनी चाहिये?कंगना ने पूरे फिल्म जगत पर ड्रग्स के गंभीर आरोप लगाये हैं और प्रत्युत्तर में उस पर भी यही आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच होना आवश्यक है। क्या कंगना को ऐसी जांच में सहयोग नही करना चाहिये? यदि उसे जांच के लिये बुलाया जाता है तो क्या उसे बदले की कारवाई कहा जाना चाहिये?
कंगाना ने महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है क्या उसका स्वागत किया जाना चाहिये? जिन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किये गये है क्या उनके आरोप और भाषा कंगना से भिन्न रहे हैं? आज जिस तरह से प्रदेश सरकार और भाजपा ने इस मामले में अपने को शामिल कर लिया है वहां पर उसके अपने ही खिलाफ दर्जनों ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि क्या सरकार और भाजपा अवैध निर्माणों के पक्ष में है।



