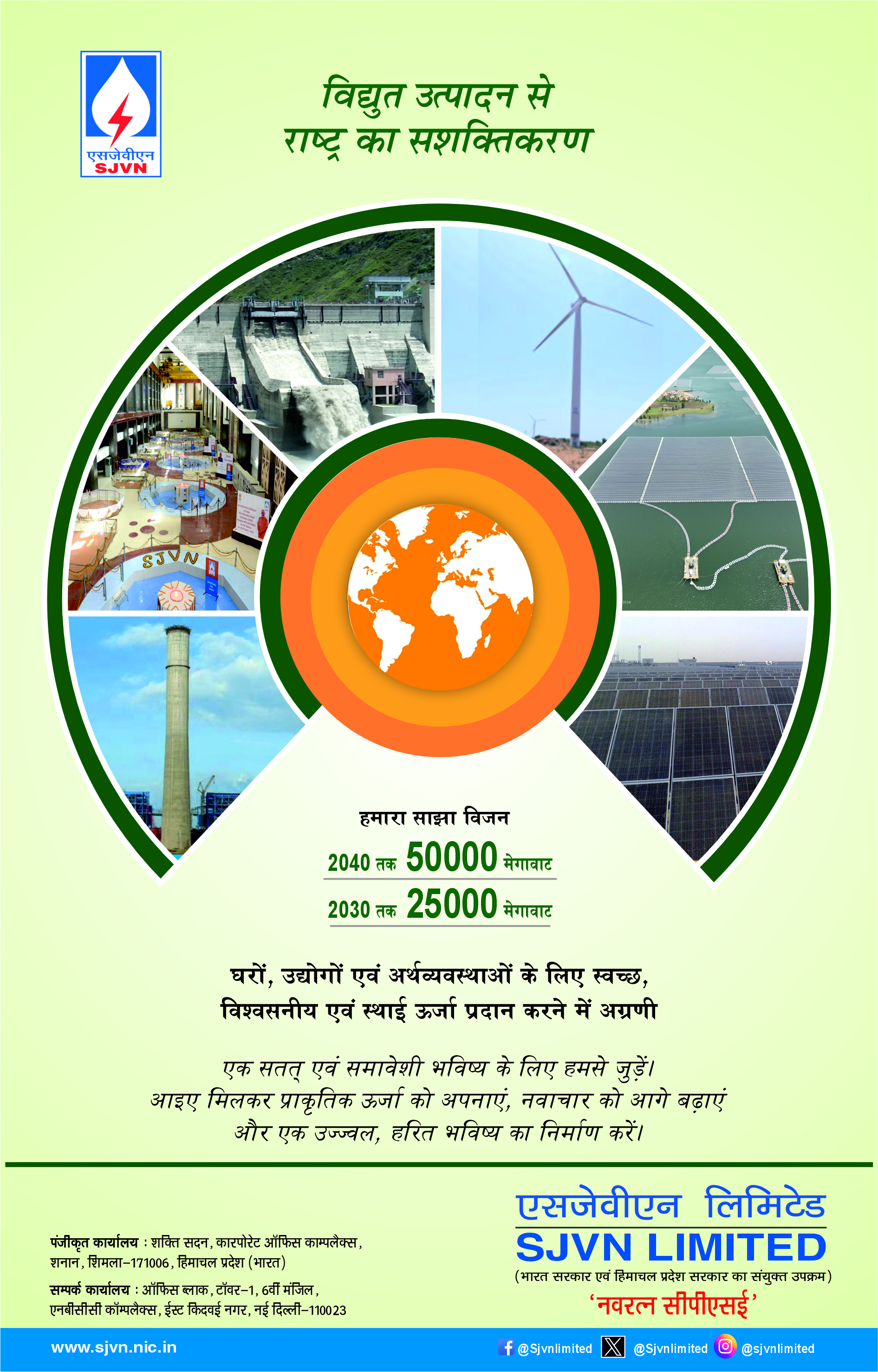ShareThis for Joomla!
गंभीर होंगे किसान आन्दोलन के परिणाम
- Details
- Created on Tuesday, 20 February 2024 10:17
- Written by Shail Samachar
 किसान फिर आन्दोलन पर हैं। इससे पहले भी तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक वर्ष भर किसान आन्दोलन पर रहे हैं। यह आन्दोलन तब समाप्त हुआ था जब प्रधानमंत्री ने यह कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसान तब तक आन्दोलन नहीं छोड़ता जब तक उसकी मांगे मान नहीं ली जाती है। इसलिये अब भी किसान अपनी मांग पूरी करवा कर ही आन्दोलन समाप्त करेंगे। पिछले आन्दोलन को दबाने, असफल बनाने के लिये जो कुछ सरकार ने किया था वही सब कुछ अब किया जा रहा है और किसान न तब डरा था और न ही अब डरेगा। इसलिये यह समझना आवश्यक हो जाता है कि किसानों की मांगे है क्या और कितनी जायज हैं। जब सरकार तीन कृषि विधेयक लायी थी तब कारपोरेट जगत के हवाले कृषि और किसान को करने की मंशा उसके पीछे थी। जैसे ही किसानों को यह मंशा स्पष्ट हुई तो वह सड़कों पर आ गया और उसका परिणाम देश के सामने है। इस वस्तुस्थिति में वर्तमान आन्दोलन को देखने समझने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार में सबसे बड़ा योगदान है। यह सरकार की हर रिपोर्ट स्वीकारती है। लेकिन इसी के साथ यह कड़वा सच है कि देश में होने वाली आत्महत्या में भी सबसे बड़ा आंकड़ा किसान का ही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जो अन्नदाता है और जिसकी भागीदारी जीडीपी और रोजगार में सबसे ज्यादा है वह आत्महत्या के कगार पर क्यों पहुंचता जा रहा है। स्वभाविक है कि सरकार की नीतियों और किसान बागवान की व्यवहारिक स्थिति में तालमेल नहीं है। आज सरकार का जितना ध्यान और योगदान कॉरपोरेट उद्योग की ओर है उसका चौथा हिस्सा भी किसान और किसानी के कोर सैक्टर की ओर नहीं है। कोरोना कॉल के लॉकडाउन में जहां उद्योग जगत प्रभावित हुआ वहीं पर किसान और उसकी किसानी भी प्रभावित हुई। कॉरपोरेट जगत को उभारने के लिये सरकार पैकेज लेकर आयी लेकिन कृषि क्षेत्र के लिये ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉरपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों का कर्ज़ बट्टे खाते में डाल दिया गया लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज जब सर्वाेच्च न्यायालय ने चुनावी चन्दा बाण्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर इस पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाते हुये चन्दा देने वालों की सूची तलब कर ली है तब यह सामने आया है कि विजय माल्या ने विदेश भागने से पहले 10 करोड़ का चन्दा भाजपा को दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का व्यवहार कॉरपोरेट घरानों के प्रति क्या है और कृषि तथा किसानों के प्रति क्या है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दो गुनी करने का वादा किया था वह कितना पूरा हुआ है वह हर किसान जानता है। किसानी बागवानी को लेकर पिछले पांच वर्षों में केन्द्र की घोषित योजनाओं का सच यह है कि कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख करोड़ से अधिक का धन लैप्स कर दिया गया है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि और किसान के प्रति सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अन्तर है। आज आन्दोलनरत किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहा है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 201 सिफारिशें की थी जिनमें से 175 पर यूपीए के काल में ही अमल हो गया था। लेकिन 26 सिफारिशों पर ही अमल बाकी है। नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कृषि का समर्थन मूल्य तय करने के लिये सूत्र दिया था आज उसी पर अमल नहीं कर पा रहें हैं। 1960 में न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक वस्तुओं के लिये लागू किया गया था। आज किसान इसी समर्थन मूल्य नियम को विस्तारित करके सारी कृषि उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। इस समर्थन मूल्य को वैधानिक कवच प्रदान करने की मांग है। यह व्यवहारिक सच है कि आज कृषि में हर चीज का लागत मूल्य कई गुना बढ़ चुका है और उसके अनुपात में किसान को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को नहीं माना तो इसके परिणाम गंभीर होंगे।
किसान फिर आन्दोलन पर हैं। इससे पहले भी तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक वर्ष भर किसान आन्दोलन पर रहे हैं। यह आन्दोलन तब समाप्त हुआ था जब प्रधानमंत्री ने यह कानून वापस लेने की घोषणा की थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसान तब तक आन्दोलन नहीं छोड़ता जब तक उसकी मांगे मान नहीं ली जाती है। इसलिये अब भी किसान अपनी मांग पूरी करवा कर ही आन्दोलन समाप्त करेंगे। पिछले आन्दोलन को दबाने, असफल बनाने के लिये जो कुछ सरकार ने किया था वही सब कुछ अब किया जा रहा है और किसान न तब डरा था और न ही अब डरेगा। इसलिये यह समझना आवश्यक हो जाता है कि किसानों की मांगे है क्या और कितनी जायज हैं। जब सरकार तीन कृषि विधेयक लायी थी तब कारपोरेट जगत के हवाले कृषि और किसान को करने की मंशा उसके पीछे थी। जैसे ही किसानों को यह मंशा स्पष्ट हुई तो वह सड़कों पर आ गया और उसका परिणाम देश के सामने है। इस वस्तुस्थिति में वर्तमान आन्दोलन को देखने समझने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार में सबसे बड़ा योगदान है। यह सरकार की हर रिपोर्ट स्वीकारती है। लेकिन इसी के साथ यह कड़वा सच है कि देश में होने वाली आत्महत्या में भी सबसे बड़ा आंकड़ा किसान का ही है। ऐसे में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जो अन्नदाता है और जिसकी भागीदारी जीडीपी और रोजगार में सबसे ज्यादा है वह आत्महत्या के कगार पर क्यों पहुंचता जा रहा है। स्वभाविक है कि सरकार की नीतियों और किसान बागवान की व्यवहारिक स्थिति में तालमेल नहीं है। आज सरकार का जितना ध्यान और योगदान कॉरपोरेट उद्योग की ओर है उसका चौथा हिस्सा भी किसान और किसानी के कोर सैक्टर की ओर नहीं है। कोरोना कॉल के लॉकडाउन में जहां उद्योग जगत प्रभावित हुआ वहीं पर किसान और उसकी किसानी भी प्रभावित हुई। कॉरपोरेट जगत को उभारने के लिये सरकार पैकेज लेकर आयी लेकिन कृषि क्षेत्र के लिये ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉरपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों का कर्ज़ बट्टे खाते में डाल दिया गया लेकिन किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज जब सर्वाेच्च न्यायालय ने चुनावी चन्दा बाण्ड योजना को असंवैधानिक करार देकर इस पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाते हुये चन्दा देने वालों की सूची तलब कर ली है तब यह सामने आया है कि विजय माल्या ने विदेश भागने से पहले 10 करोड़ का चन्दा भाजपा को दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का व्यवहार कॉरपोरेट घरानों के प्रति क्या है और कृषि तथा किसानों के प्रति क्या है। प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दो गुनी करने का वादा किया था वह कितना पूरा हुआ है वह हर किसान जानता है। किसानी बागवानी को लेकर पिछले पांच वर्षों में केन्द्र की घोषित योजनाओं का सच यह है कि कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख करोड़ से अधिक का धन लैप्स कर दिया गया है। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि और किसान के प्रति सरकार की कथनी और करनी में दिन रात का अन्तर है। आज आन्दोलनरत किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहा है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 201 सिफारिशें की थी जिनमें से 175 पर यूपीए के काल में ही अमल हो गया था। लेकिन 26 सिफारिशों पर ही अमल बाकी है। नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कृषि का समर्थन मूल्य तय करने के लिये सूत्र दिया था आज उसी पर अमल नहीं कर पा रहें हैं। 1960 में न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक वस्तुओं के लिये लागू किया गया था। आज किसान इसी समर्थन मूल्य नियम को विस्तारित करके सारी कृषि उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। इस समर्थन मूल्य को वैधानिक कवच प्रदान करने की मांग है। यह व्यवहारिक सच है कि आज कृषि में हर चीज का लागत मूल्य कई गुना बढ़ चुका है और उसके अनुपात में किसान को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसे में यदि सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को नहीं माना तो इसके परिणाम गंभीर होंगे।
कांग्रेस को अपनों से ही खतरा है
- Details
- Created on Friday, 09 February 2024 12:55
- Written by Shail Samachar

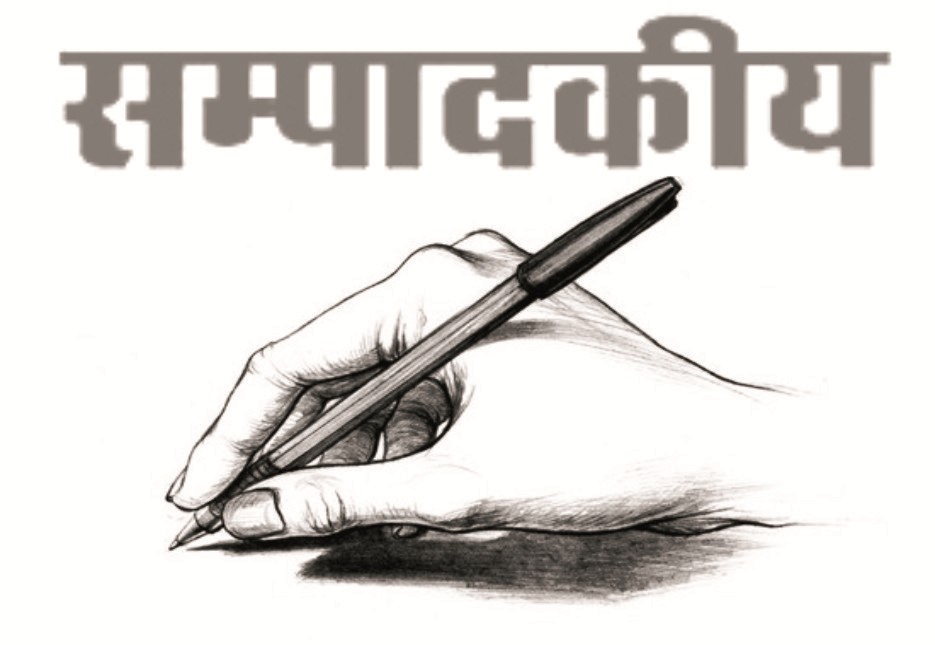
क्या मोदी ‘‘राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा’’ के बाद भी शंकित है
- Details
- Created on Monday, 05 February 2024 15:58
- Written by Shail Samachar




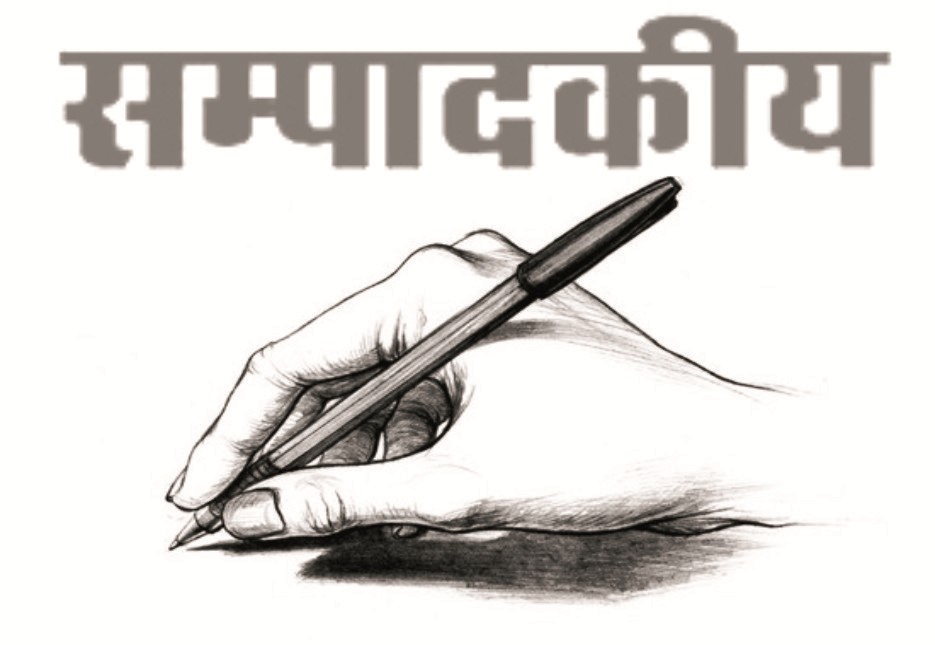
लेकिन यह भी एक प्रमाणित सच है कि रात चाहे कितनी भी काली और लम्बी क्यों न हो पर सवेरा आकर ही रहता है। इस समय सारे गंभीर प्रश्नों से ध्यान हटाने का जो प्रयोग धर्म और जातियों में आपसी टकराव खड़ा करके किया जा रहा था उसका एक चरम अभी राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में सामने आ चुका है। इस आयोजन पर शंकराचार्यों से लेकर अन्य विश्लेषको ने जो सवाल उठाये हैं उससे शायद सत्ता को कुछ झटका लगा है। इसलिये इस आयोजन के बाद राहुल गांधी के न्याय यात्रा को असफल करने के लिये हर राज्य में अड़चने पैदा करने का प्रयास किया गया है। इसी के लिये ‘‘इण्डिया’’ गठबन्धन को तोड़ने के सारे प्रयास शुरू हो गये हैं। जिस तरह से गठबन्धन के बड़े घटक दल अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस को सीटे देने के लिये तैयार नही हो रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि चुनावों से पहले ही यह गठबन्धन दम तोड़ देगा। सभी दल अलग-अलग चुनाव लड़ने की बाध्यता पर आ जायेंगे।
राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन ने हर दल को प्रभावित किया है। बल्कि हर दल में वह लोग स्पष्ट रूप से चिन्हित हो गये हैं जो धर्म की राजनीति में संघ भाजपा के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। ऐसे में यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि जो राजनीतिक लोग या दल धर्म और राजनीति में ईमानदारी से अन्तर मानते हैं उन्हें बड़े जोर से यह कहना पड़ेगा की राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हुआ है वह शुद्ध रूप से संघ भाजपा का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। इस आयोजन के बाद भाजपा के ही अन्दर उठने वाले सवालों को लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर चुप करवाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस आयोजन के बाद जो कुछ बिहार, झारखण्ड और चण्डीगढ़ में घटा है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि मोदी अभी भी शंकित हैं कि क्या अकेला राम मन्दिर ही उनको सफलता दिला पायेगा? इसी शंका ने उनको ‘‘इण्डिया’’ को तोड़ने के प्रयासों में लगा दिया है। ‘‘इण्डिया’’ में नीतीश कुमार, ममता बैनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल की सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह का आचरण सामने आ रहा है उसका भाजपा और कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर अगले अंक में आकलन किया जायेगा। लेकिन जो कुछ मोदी ने किया है वहां निश्चित रूप से उनके डर का ही प्रमाण है।
क्या राम मन्दिर असफलताओं को छुपाने का माध्यम बनेगा?
- Details
- Created on Sunday, 28 January 2024 11:39
- Written by Shail Samachar




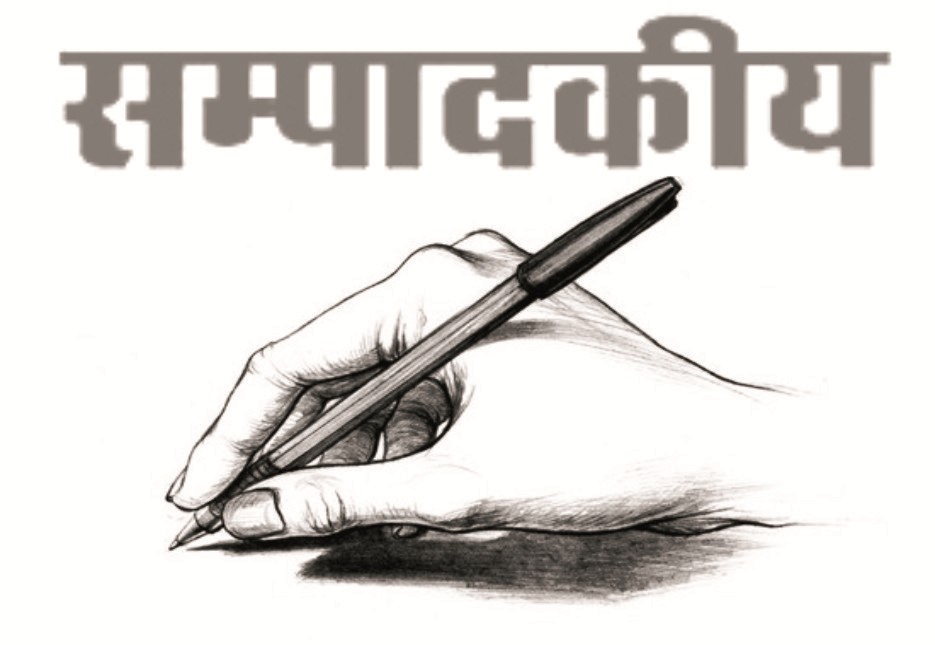
राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के शीर्ष धर्मगुरुओं चारों शंकराचार्यों ने यह सवाल उठाया था कि अधूरे मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ऐसा करना कई अनिष्टों का कारण बन जाता है। शंकराचार्यों का यह प्रश्न इस आयोजन में अनुत्तरित रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह सवाल हर गांव में उठेगा। क्योंकि हर जगह मन्दिर निर्माण होते ही रहते हैं। इसी आयोजन में प्राण प्रतिष्ठा से पहले साढ़े सात करोड़ से निर्मित दशरथ दीपक का जलकर राख हो जाना क्या किसी अनिष्ट का संकेत नहीं माना जा सकता? स्वर्ण से बनाये गये दरवाजे पर उठे सवालों को कितनी देर नजरअन्दाज किया जा सकेगा? प्राण प्रतिष्ठा के बाद शीशे का न टूटना सवाल बन चुका है। आज मौसम जिस तरह की अनिष्ट सूचक होता जा रहा है क्या उसे आने वाले दिनों में अतार्किक आस्था अगर इन सवालों का प्रतिफल मानने लग जाये तो उसे कैसे रोका जा सकेगा। हिन्दू एक बहुत बड़ा समाज है जिसमें मूर्ति पूजक भी हैं और निराकार के पूजक भी हैं। राम की पूजा करने वाले भी हैं और रावण के पूजक भी हैं। आर्य समाज ने तो हिन्दू धर्म के समान्तर एक अपना समाज खड़ा कर दिया है। आर्य समाजियों के अनुसार वेद का कोई मन्त्र यह प्रमाणित नहीं करता कि मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं? राधा स्वामी कितना बड़ा वर्ग है क्या उसे राम की मूर्ति की पूजा के लिये बाध्य किया जा सकता है। संविधान निर्माता डॉ. अम्बेदकर क्यों बौद्ध बने थे? ऐसे अनेकों सवाल हैं जो इस आयोजन के बाद उठेंगे उसमें हिन्दू समाज की एकता पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा यह देखना रोचक होगा।
इस आयोजन ने हर राजनीतिक दल और नेता को इसमें एक पक्ष लेने की बाध्यता पर लाकर खड़ा कर दिया है। यही इस आयोजन के आयोजकों की सफलता रही है। इस आयोजन के बाद लोकसभा का चुनाव समय से पूर्व करवाने के संकेत स्पष्ट हो चुके हैं। इस चुनाव में राम मन्दिर निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को केन्द्रिय मुद्दा बनाया जायेगा। सारे सवालों को नजर अन्दाज करते हुये प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम देना प्रधानमंत्री की बड़ी उपलब्धि माना जायेगा। इस उपलब्धि के साये में देश की आर्थिकी, बेरोजगारी और महंगाई पर उठते सवालों को राम विरोध करार दिया जायेगा। जिन गैर भाजपा राज्य सरकारों ने इस आयोजन के दौरान भाजपा की तर्ज पर ही कई कार्यक्रम और आयोजन आयोजित किये हैं वह लोकसभा चुनावों में भाजपा को मात दे पाते हैं या देखना भी रोचक होगा। क्योंकि हर सरकार राम मन्दिर के आचरण में अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास करेंगे।
‘‘सरकार गांव के द्वार’’ कितना सार्थक होगा यह प्रयोग
- Details
- Created on Sunday, 21 January 2024 18:02
- Written by Shail Samachar




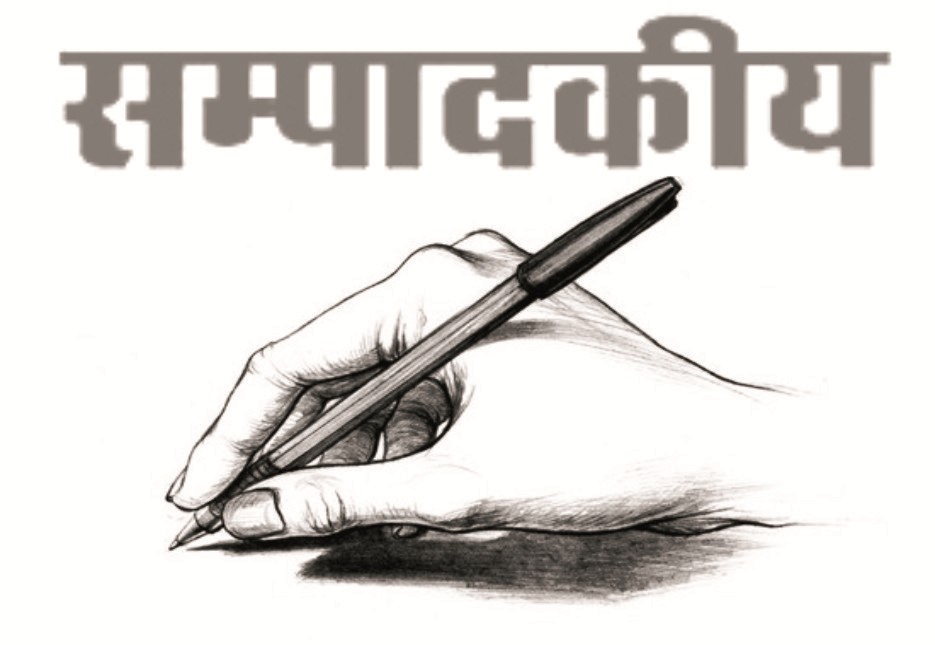
इस समय ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत पिछले दिनों आयोजित की गयी राजस्व लोक अदालतों के लाभार्थी और आपदा में मकान आदि के लिये मिलने वाली आर्थिक सहायता पाने वाले दो वर्ग ही सामने आ रहे हैं। जबकि राजस्व अदालतों में इंतकाल आदि के लंबित मामले शुद्ध रूप से प्रशासनिक असफलता का प्रमाण है। यह अदालत आयोजित करके लोगों को राहत देने से ज्यादा भ्रष्ट तंत्र को ढकने का ज्यादा प्रयास है। क्योंकि क्या हर सरकार ऐसे मामलों को निपटाने के लिये ऐसी अदालतें आयोजित करके अपनी पीठ थपथपाती रहेगी। इसके लिये स्थायी व्यवस्था कौन करेगा। कायदे से तो ऐसे तंत्र के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जानी चाहिये थी। पिछले दिनों प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक दायित्व के साथ ही न्यायिक कार्य कर रहे अधिकारियों के काम काज पर जब अप्रसन्नता व्यक्त की तब सरकार ने यह आयोजन शुरू किया।
आज हिमाचल के लिये कर्ज और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रदेश का जो कर्ज भार 2013-14 में 31442.56 करोड़ दिखाया गया था वह आज एक दशक में एक लाख करोड़ के पास क्यों पहुंच गया है। यह सारा कर्ज विकास कार्यों के नाम पर लिया गया है क्योंकि राजस्व व्यय के लिये सरकारें कर्ज नहीं ले सकती। क्या सरकार अपने कार्यक्रमों में जनता को यह जानकारी देगी कि यह कर्ज कौन से कार्यों के लिये लिया गया और उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है। इस समय जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग कर दिया गया था उसकी जे.ओए.आई.टी. कोड की परीक्षा पास किये हुये बच्चे पिछले चार वर्षों से परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे अब यह मांग करने पर आ गये हैं कि ‘हमें नौकरी दो या जहर दे दो’। क्या सरकार गांव के द्वार पर जाकर इन बच्चों और उनके अभिभावकों के प्रश्नों का जवाब दे पायेगी? इसी तरह एस.एम.सी. शिक्षकों और गेस्ट टीचरों के मसलों पर जनता का सामना कर पायेगी? यही स्थिति मल्टीपरपज के नाम पर भर्ती कियें गये 6000 युवाओं की है क्या वह 4500 रुपए में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पायेंगे? क्या इन सवालों को केंद्र से सहायता न मिल पाने के नाम पर लम्बे समय के लिये टाला जा सकेगा? क्या जनता इन सवालों पर मुख्य संसदीय सचिवों और एक दर्जन से अधिक सलाहकारों और विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्तियों के औचित्य पर सवाल नहीं पूछेगी?