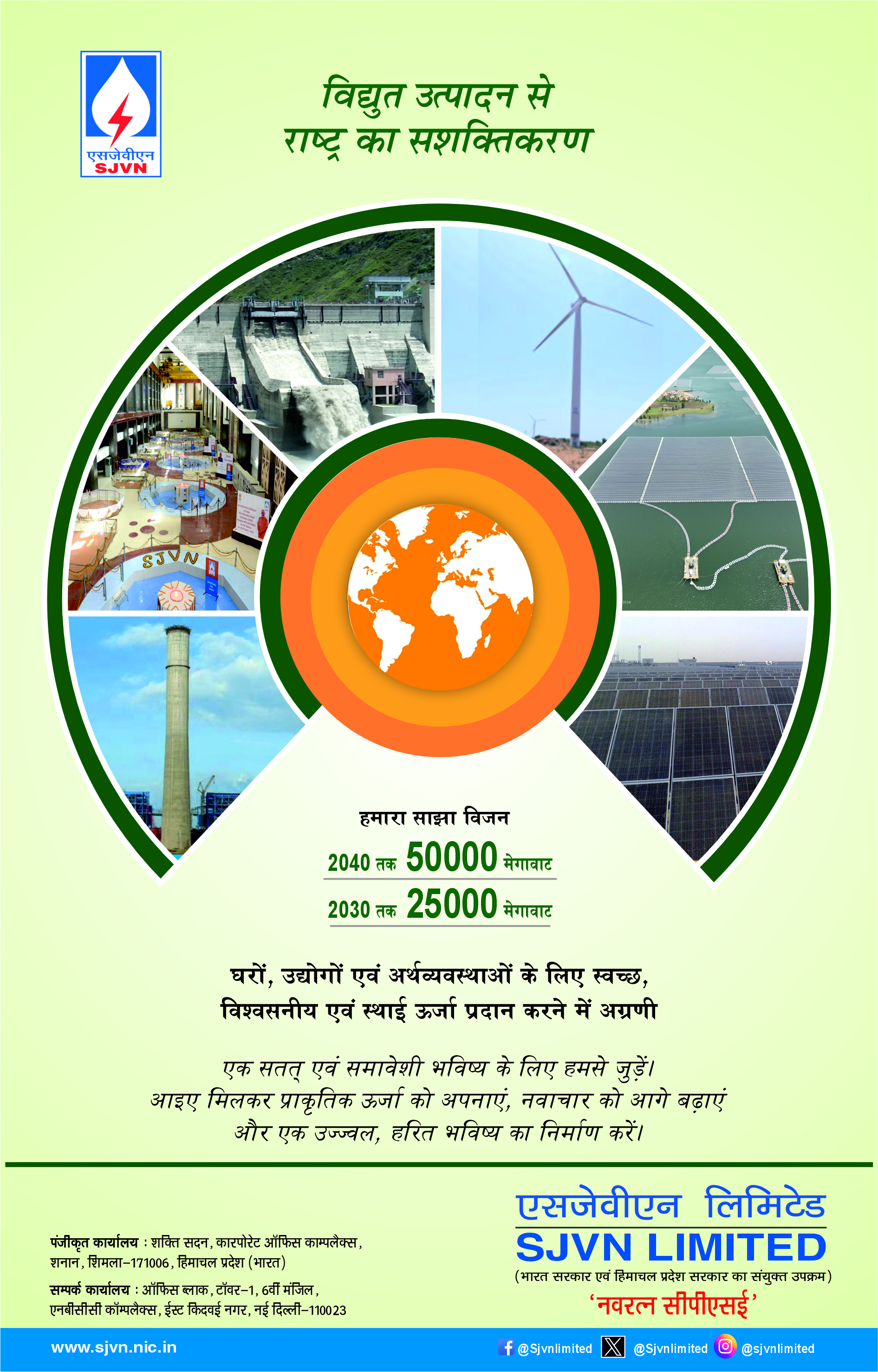ShareThis for Joomla!
चुनाव सुधारों को टालना घातक होगा
- Details
- Created on Tuesday, 31 January 2017 08:09
- Written by Shail Samachar
शिमला/बलदेव शर्मा अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन राज्यों में इस समय उत्तराखण्ड में कांग्रेस, पंजाब में अकाली -भाजपा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में है। इन चुनावों में यह सभी दल फिर से चुनाव मैदान में कहीं सीधे तो कहीं गठबन्धन की शक्ल मे इनके अतिरिक्त बसपा और ‘‘आप’’ भी चुनाव में है। बसपा यूपी में पहले भी सरकार चला चुकी है और आप दिल्ली में सरकार चला रही है। भाजपा के पास इस समय केन्द्र सरकार है तो कांग्रेस के पास इससे पहले रह चुकी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी दलों को सरकार चलाने का अनुभव है और सभी को सरकारों की वित्तिय स्थिति तथा जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं का भी ज्ञान है। इसी के साथ यह भी एक सच है कि सभी राज्य सरकारें कर्ज के बोझ तले भी है और यह कर्ज हर वर्ष घटने की बजाये बढ़ता ही जा रहा है सभी को राज्यों के संसाधनों का भी पता है। लेकिन आज यदि इन सभी दलों के वर्तमान और पूर्व के चुनाव घोषणा पत्रों का एक निष्पक्ष आकलन किया जाये तो जो तस्वीर उभरती है वह एकदम चिन्ताजनक और निराशाजनक दिखती है। क्योंकि किसी के भी घोषणापत्र में संसाधनों का जिक्र नही है। किसी ने भी संबंधित राज्य की आर्थिक और वित्तिय स्थिति का कोई उल्लेख नही किया है। सभी ने जनता को अधिक से अधिक मुफत लाभ देने का वायदा किया है बल्कि इन घोषणापत्रों को देखकर तो यह सवाल भी उठता है कि जो वायदे इस बार किये जा रहें है क्या जनता की यह आवश्यकताएं अभी पैदा हुई है? जब यह दल सरकार चला रहे थे क्या तब जनता को इस सबकी आवश्यकता नही थी? कुल मिलाकर सभी दलों के घोषणपत्रों को प्रलोभनों का पिटारा और मतदाताओं को खरीदने का प्रयास करार दिया जा सकता हैं। कहीं भी यह नही बताया गया है कि इन वायदों को पूरा करने के लिये साधन कहां से आयेंगे? यह वायदा नहीं किया गया है कि जनता पर परोक्ष/अपरोक्ष में कोई नया टैक्स नही लगाया जायेगा और न ही सरकार पर कर्ज का बोझ डाला जायेगा। यदि ईमानदारी से आंकलन किया जाये तो सभी के घोषणापत्र आचार संहिता का उल्लघंन करार दिये जा सकते है।
लेकिन हमारा चुनाव आयोग इस बुनियादी पक्ष की ओर एकदम आंख बन्द करके बैठा हुआ है। हर बार चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी जाती है और इसमें भी राजनीतिक दलों पर तो कोई सीमा है ही नही। राजनीतिक दलों की आय के स्त्रोत कितने वैध हैं और कितने अवैध इसका खुलासा सामने आ चुका है। राजनीतिक दलों की 69 प्रतिशत आय अज्ञात स्त्रोतों से है जिसे सीधे-सीधे अवैध करार दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास इतनी आय अज्ञात स्त्रोतांे से हो तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला बन जाता है और सज़ा मिलती है। लेकिन राजनीतिक दलों को लेकर न्यायपालिका और चुनाव आयोग दोनों ही एकदम पंगु होकर बैठे हुए है। क्योंकि यह घोषणापत्र जनता का ऐजैन्डा न होकर इन दलों की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने का ऐजैन्डा होकर रह गये है। गरीबों को कुछ चीजे सस्ते में या मुफत उपलब्ध करवा कर एक निश्चित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना स्वस्थ लोकतन्त्र का मानक नही माना जा सकता। चुनावों की यह वर्तमान व्यवस्था धीरे - धीरे अपराधियों, धनबलियों और बाहुबलियों को शासन के शीर्ष पर बैठाने का साधन होकर रह गयी है। आज राजनीतिक दल पेशेवर चुनाव प्रबन्धकों और प्रचारको के रोजगार का एक बड़ा स्त्रोत बन कर रह गये है। राजनीतिक दल कारपोरेट संस्कृृति का पर्याय बनकर रह गये हैं। कोई भी दल राजनीति में बढते अपराधीकरण को लेकर अपने घोषणापत्रों में एक शब्द तक नही कह पाया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज राजनीतिक दलों का एक मात्र सरोकार सत्ता में बने रहने के अतिरिक्त और कुछ नही रह गया है। ऐसे में यह सोचना पडे़गा कि यदि ही चुनावी व्यवस्था चलता रही तो निकट भविष्य में स्थितियां कहां से कहां पहुंच जायेगी।
इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है। कि समय रहते ही चुनावी व्यवस्था और इससे वांच्छित सुधारों को लेकर एक सर्वाजनिक बहस शुरू की जायेे। राजनीतिक दलों और जनता के बीच एक सशक्त संवाद कैसे स्थापित हो सकता है। इसके लिये कौन सा मंच कारगर हो सकता है? इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। चुनाव को धनबल और बाहुबल से कैसे मुक्त रखा जाये? क्योंकि इस वक्त जिस तरह का चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें तो जनता को सोचने विचारने का समय ही नहीं मिल पाता है। आज की व्यवस्था में राजनीतिक दल और राजनेता को सुनने की व्यवस्था तो है। परन्तु उसे सुनाने और उससे पूछने की कोई तय व्यवस्था नही है। आज माॅडल आचार संहिता तो है परन्तु उसकी अवहेलना पर दण्डनीय अपराध दर्ज हो पाने का प्रावधान नही है इस पर केवल चुनाव परिणाम के बाद चुनाव याचिका दायर करने का ही प्रावधान है। इसलिये आज आवश्वकता है कि जनता और रानीतिक दल तथा राजनेता के बीच अधिकाधिक संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। क्योंकि सैद्धान्तिक रूप से तो चुनाव प्रचार का अर्थ ही मतदाताओं के साथ सार्थक संवाद की स्थापना है और यह संवाद लगभग बिना किसी बड़े खर्च से स्थापित किया जा सकता है। इसके लियेे सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका तीनों को अपने- अपने स्तर पर प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते यह न हो पाया तो बहुत संभव है कि जनता स्वयं को ऐसा कुछ करने पर आ जाये जो अराजकता की सीमा तक जा पहुंचें।